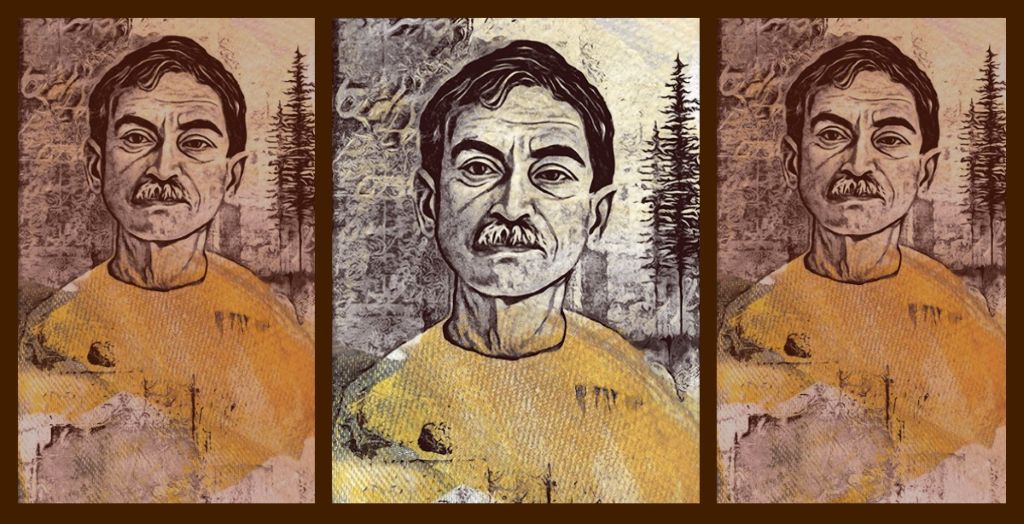उपन्यास-सम्राट मुंशी प्रेमचंद, निस्संदेह, हिंदी के उन गिने-चुने कथाकारों में से एक हैं, जिनके साहित्य का भरपूर अवगाहन हुआ है. उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी. हां, इस बहुविध अवगाहन ने बहुत-सी क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं को भी जन्म दिया है. इस लिहाज से उन्हें उनके सृजन ही नहीं, जीवन के आईने में देखना भी दिलचस्प है. उन छोटे-छोटे निजी प्रसंगों और वाकयों में भी, जिन्हें कई बार ‘इधर उधर से लिया गया’ और इस कारण महत्वहीन समझकर दरकिनार कर दिया जाता है.
उनके बारे में बहुप्रचारित तथ्य है कि आजादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन के वक्त आठ फरवरी, 1921 को महात्मा गांधी गोरखपुर आए तो बीमार होने के बावजूद वे उनको सुनने गए और उनकी कही बातों पर चिंतन-मनन के हफ्ते भर बाद 16 फरवरी को शिक्षा विभाग की अपनी जमी-जमाई सरकारी नौकरी छोड़ दी. इसके कुछ दिनों बाद जीविकोपार्जन के लिए करघे का कारखाना खोला तो उसे चला नहीं पाए.
खूबियों पर सबका हक
1930 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने बनारस से ‘हंस’ नामक साहित्यिक पत्र निकालना शुरू किया और उसके संपादक ही नहीं पीर-बावर्ची-खर सब बन गए तो कहते हैं कि पत्नी शिवरानी देवी द्वारा निजी जरूरतों के लिए उन्हें दिए रुपये भी वे कई बार ‘हंस’ के ‘कहीं ज्यादा जरूरतमंद’ कर्मचारियों को दे देते थे.
हंस से जुड़ा एक और किस्सा यों है कि उस वक्त के एक ऐसे चर्चित लेखक ने, जो एक ओर तो अपने लिखे उत्कृष्ट नाटकों लिए जाने जाते थे और दूसरी ओर फरेब रचने और लोगों को उल्लू बनाने के आरोपों के शिकार थे, ‘हंस’ के लिए अपनी रचनाएं भेजनी शुरू कीं. तब प्रेमचंद ऐसी सूचनाओं के बावजूद उनकी रचनाएं छापते रहे कि फरेबों के आरोपों से उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है और अनेक लोग उनके निकट आने के बजाय उनसे दूर-दूर रहना ही पसंद करने लगे हैं.
एक दिन जब प्रेमचंद ‘हंस’ के कार्यालय में बैठे कोई काम निपटा रहे थे, उनके एक सहयोगी ने अचानक इस बारे में उनसे पूछ लिया, ‘आप ऐसे लेखक को ‘हंस’ में बार-बार इतनी जगह कैसे दे सकते हैं, जो रोज-रोज लोगों को ठगने के नए-नए बहाने बनाता रहता है? देख लीजिएगा, अवसर हाथ आते ही, वह आपको भी ठगने से बाज नहीं आएगा. उसकी रचनाएं छपने से ‘हंस’ का नाम भी खराब हो ही रहा है.’
प्रेमचंद का जवाब था, ‘कह तो तुम ठीक ही रहे हो. वह ठग भी है, झूठा भी, प्रपंची भी और मक्कार भी.’
इससे सहयोगी को लगा कि उन्होंने उसकी बात मान ली है और आगे उस लेखक की रचनाओं को ‘हंस’ में कभी भी कतई जगह नहीं देंगे. लेकिन अगले ही पल प्रेमचंद ने उसको सवालों के सामने करते हुए कहा, ‘मगर एक बात बताओ, क्या इतनी-सी बात के लिए ‘हंस’ के पाठकों को इस लेखक के अद्भुत लेखन से वंचित करना उचित होगा? क्या तुम चाहते हो कि उसकी बुरी आदतों की सजा उसकी लेखन प्रतिभा को नकार कर दिया जाए?’
बेचारा सहयोगी क्या जवाब देता? पल भर उसके जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद प्रेमचंद ही फिर बोले,
‘हम ‘हंस’ के पाठकों को अच्छी रचनाओं से वंचित रखने का पाप नहीं कर सकते. हमारा काम है पाठक को बेहतर रचनाएं देना. फिर किसी भी व्यक्ति की, वह कैसा भी क्यों न हो, खूबियों पर समाज का अधिकार होता है और उन्हें उनकी सही जगह मिलनी ही चाहिए.’
कई लोग इस प्रसंग की बिना पर कहते हैं कि प्रेमचंद किसी व्यक्ति के जीवन और साहित्य को अलग-अलग देखने के पक्षधर थे.
आजादी की जंग में
बहरहाल, उनके द्वारा संपादित व प्रकाशित मासिक ‘हंस’ और साप्ताहिक ‘जागरण’ दोनों गवाह हैं कि इन पत्रों में छपी टिप्पणियों, लेखों व संपादकीयों की मार्फत देश की तत्कालीन गोरी सत्ता को चुनौती देकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा. जुर्माना व जमानत मांगे जाने के जोखिम भी उठाए और पुराने मूल्यों की जगह नए मूल्यों व संस्कारों को प्रतिष्ठित करने के संघर्ष भी किए.
‘हंस’ के प्रकाशन से छह महीने पहले उन्हें उसका नाम उनके अभिन्न जयशंकर प्रसाद ने सुझाया था. तब प्रसाद को एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं कोई धनी व्यक्ति नहीं बल्कि मजदूर आदमी हूं, लेकिन ‘हंस’ निकालने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि काशी से कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं निकलती. जाहिर है कि वे इस अभाव की पूर्ति करना चाहते थे. इसीलिए उसके पहले अंक के संपादकीय में लिखा था कि हंस भी अपनी नन्हीं चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिए हुए समुद्र पाटने, आजादी की जंग में योगदान देने चला है… साहित्य और समाज में वह उन गुणों का परिचय करा ही देगा, जो परंपरा ने उसे प्रदान किया है.
इससे पहले अपने घनिष्ठ मित्र दयानारायण निगम (जिन्होंने सोजे वतन पर सरकारी कोप के बाद उन्हें नवाब राय के बजाय प्रेमचंद नाम से लिखने का मशवरा दिया था) द्वारा संपादित ‘जमाना’ नामक पत्र में लिखी उनकी शुरुआती टिप्पणियों में भी वे अपने इन्हीं गुणों का परिचय कराते हैं.
ठीक है कि वे आजकल प्रचलित अर्थों में स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन पाए, पर अपने उपन्यासों व कहानियों ही नहीं, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों व संपादकीयों के जरिये उन्होंने आजादी के सवाल को न सिर्फ खासा तीखा किया बल्कि उसके लिए संघर्षरत नायकों में विद्रोह की चेतना जगाईं. तभी से जब वे प्रेमचंद नहीं बने थे.
3 जून, 1932 को बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा गया उनका वह पत्र भी यही कहता है, जिसमें यह लिखते हुए कि ‘मेरी आकांक्षा बहुत ज्यादा नहीं है. खाने भर को मिल जाता है. मुझे दौलत-शोहरत नहीं चाहिए.’ उन्होंने बताया है कि मैं चाहता हूं कि तीन-चार ऐसी अच्छी पुस्तकें लिख सकूं, जो आजादी के काम आ सके. इससे पहले अप्रैल, 1932 के ‘हंस’ में प्रकाशित ‘दमन की सीमा’ शीर्षक संपादकीय को लेकर उनसे एक हजार रुपये की जमानत मांगी गयी थी, जिसके बाद उन्हें ‘हंस’ को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा था.
चोंचलों से क्या काम?
एक और वाकये के ज़िक्र से पहले जान लेना चाहिए कि उनके वक्त में निब लगे ऐसे कलम इस्तेमाल किए जाते थे, उनसे लिखने से पहले जिनकी निबों को स्याही भरे दवात में डुबोना पड़ता था. वे ऐसा करते तो जानें कैसे कुछ स्याही उनके होठों पर भी लग जाती. उनके आस-पास के लोग उनसे इसका कारण पूछना तो चाहते, मगर संकोचवश पूछ नहीं पाते.
लेकिन एक दिन एक कार्यक्रम में एक युवक ने पूछ ही लिया. अलबत्ता, सवाल का रूप थोड़ा बदलकर, ‘आप कैसे कागज पर और किस तरह के कलम से लिखते हैं?’
प्रेमचंद ने हंसकर उसे बताया, ‘सादे कागज पर, ऐसे पेन से, जिसकी निब टूटी हुई न हो. मैं कलम का मजदूर हूं भाई. ऐसे चोंचलों से कतई काम नहीं लेता कि खास तरह के कलम और कागज हों, तभी लिखने का मूड बने.’
अलबत्ता, इसके बाद उन्होंने हैरान युवक को यह भी बता दिया कि लेखन के वक्त कभी-कभी, जब वे गहन चिंतनरत होते हैं, आदतन, उनके कलम की निब उनके दांतों तक चली जाती है, जिससे उसकी कुछ स्याही उनके होंठों पर लग जाती है. लेकिन इससे बचने के लिए वे अपनी एकाग्रता से समझौता नहीं कर सकते.
उनकी पत्नी शिवरानी देवी की ‘प्रेमचंद : घर में’ नामक पुस्तक प्रकाशित होने से पहले उनके निजी या कि घरेलू जीवन के बारे में उनके पाठकों व प्रशंसकों को बहुत कम जानकारियां थीं. यह पुस्तक आई तो उनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करके उनके वृहत् पाठक व प्रशंसक समुदाय के सामने ले आई.
बताते हैं कि प्रेमचंद शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तो एक दिन इंस्पेक्टर उनके नियंत्रण वाले एक स्कूल में मुआयना करने आया. उन्होंने उसे निष्ठापूर्वक मुआयना कराया और अगले दिन छुट्टी हो जाने के बाद इत्मीनान की सांस मिली तो घर चले गए. अपने घर पर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली. जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, इंस्पेक्टर को लगा कि वे उसकी गाड़ी देखेंगे तो कुर्सी से उठकर उसे सलाम करेंगे. लेकिन उन्होंने देखकर भी अनदेखी कर दी और कुर्सी से हिले तक नहीं.
इससे खफा इंस्पेक्टर ने व देखा न ताव, गाड़ी रुकवाकर अर्दली भेजकर उन्हें बुलवाया और बेहद सख्त लहजे में पूछा कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकलता तो तुम इतने घमंड में चूर रहते हो कि उसे सलाम तक नहीं करते.
इस पर प्रेमचंद का जवाब था, ‘जब तक मैं ड्यूटी पर रहता हूं, तब तक ही नौकर रहता हूं. बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूं.’
लेखक, गुलाम और भगवान
एक बार उनके एक लेख से हिंदू सभाई बहुत नाराज हो गए. तब शिवरानी के यह पूछने पर कि आप ऐसा लिखते ही क्यों है कि लोग भड़ककर आपके दुश्मन बन जाते हैं,
उनका जवाब था: ‘लेखक को पब्लिक और गर्वनमेंट दोनों अपना गुलाम समझती हैं. आखिर लेखक भी कोई चीज़ है. वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक कैसा? लेखक का अपना अस्तित्व है. गवर्नमेंट जेल में डालती है, पब्लिक मारने की धमकी देती है, इससे लेखक डर जाए और लिखना बंद कर दे?’
एक और वाकये के मुताबिक किसी दिन किसी बात पर शिवरानी ने भगवान का नाम लिया तो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान मन का भूत है, जो इंसान को कमजोर कर देता है. स्वावलंबी मनुष्य ही की दुनिया है. अंधविश्वास में पड़ने से तो रही-सही अक्ल भी चली जाती है.
इस पर ऐतराज़ जताते हुए वे बोलीं कि मगर गांधी जी तो दिन-रात ‘ईश्वर-ईश्वर’ चिल्लाते रहते हैं, तो प्रेमचंद का उत्तर था: वे देख रहे हैं कि जनता अभी बहुत सचेत नहीं है. वह सदियों से भगवान पर विश्वास किए चली आ रही है और एकाएक अपने विचार बदल नहीं सकती. अगर एकाएक जनता को कोई भगवान से अलग करना चाहे तो यह संभव भी नहीं. इसी से वे भी शायद भगवान का ही सहारा लेकर चल रहे हैं.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)