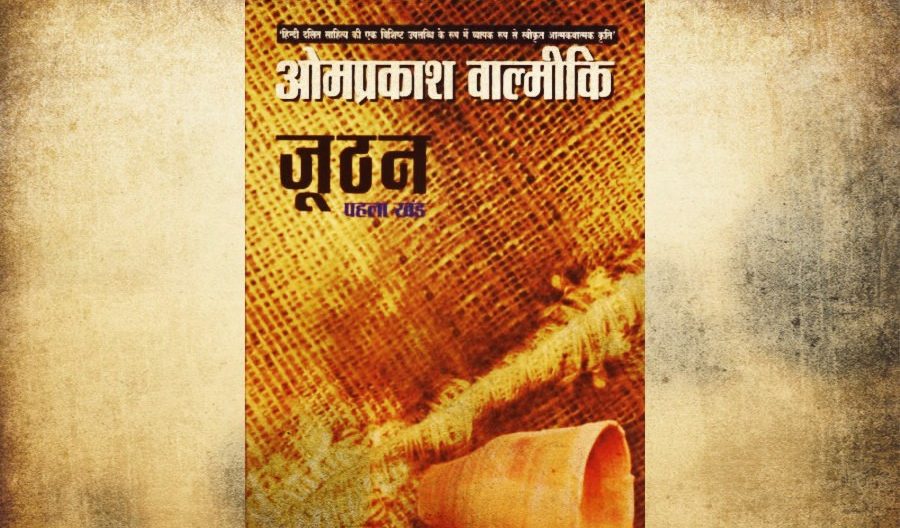हिमाचल विश्वविद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ‘जूठन’ बीते 3 सालों से पढ़ाई जा रही थी, तब भावनाएं अचानक कहां से आहत हो गईं? क्या इसका ताल्लुक़ राज्य में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन से है?

देश के 13 से अधिक विश्वविद्यालयों में-जिनमें से कई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं- फिलवक्त पढ़ायी जा रही ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ क्या रफ्ता-रफ्ता पाठ्यक्रमों से बाहर कर दी जाएगी? यह मसला अचानक सुर्खियों में आता दिख रहा है, जबसे हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में उसे लेकर अचानक हलचल मचती दिखी है.
मालूम हो कि इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के कुछ अंश हिमाचल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में कुछ साल से पढ़ाए जा रहे हैं. पिछले दिनों यह समाचार छपा कि उपन्यास पढ़ाते वक्त कुछ अध्यापकों ने अपने आपको ‘असहज’ महसूस किया और उसके ‘आपत्तिजनक’ अंशों को हटाने की उन्होंने मांग की. और अपनी इस मांग के समर्थन में वह दलाई लामा से भी मिलने गए.
मामला यहीं नहीं समाप्त हुआ. राज्य में सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन की तरफ से भी इस मांग की ताईद की गयी. राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा है कि ‘मामले की जांच करवाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे हटा दिया जाएगा.’
जानकार बता सकते हैं कि किसी किताब को पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं, बातें की जाती है. याद रहे कि किस तरह बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित, काॅमनवेल्थ रायटर्स की तरफ से पुरस्कृत उपन्यास ‘सच अ लॉन्ग जर्नी’- जो मुंबई विश्वविद्यालय के बीए इंग्लिश के छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, रातों रात पाठ्यक्रम से हटा दी गयी थी, जब शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने किताब पर सवाल उठाए थे और विश्वविद्यालय के गेट पर किताब की कॉपी जला दी थी.
या किस तरह एके रामानुजम का बहुचर्चित लेख ‘थ्री हंडरेड रामायणास’ – जिसमें रामायण की देश और बाकी हिस्सों में चल रही तीन सौ अलग अलग गाथाओं का वर्णन किया गया था – दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से इसी तरह हटा दिया गया था, जब दक्षिणपंथी संगठनों ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी.
‘सच अ लॉन्ग जर्नी’ को हटा देने के बाद एक अग्रणी लेखक समूह द्वारा जारी किया गया बयान आज अधिक मौजूं जान पड़ता दिख रहा है.
‘भारत एक प्रतियोगितात्मक लोकरंजनवाद के गर्त में फंसता दिख रहा है, जहां आहत धार्मिक, नस्लीय या क्षेत्राीय संवेदनशीलताओं के नाम पर राजनीतिक ताकतें साहित्य, कला, रंगमंच या सिनेमा जैसी रचनाओं को नष्ट करने या बंद करने में आपस में होड़ मचाती दिख रही हैं…’
(India has lapsed into the worst kind of competitive populism, with political forces seeking to outdo one another in destroying and banning works of literature, art, theatre and cinema, in the name of an aggrieved religious, ethnic or regional sensibility….)
पेरुमल मुरुगन या हांसदा सोवेंद्र शेखर के बाद अब लगता है कि ओमप्रकाश वाल्मीकि की बहुचर्चित आत्मकथा ‘जूठन’ निशाने पर है.
गनीमत समझी जाएगी कि जहां पेरुमल मुरुगन की हिमायत में पूरी लेखक आबादी खड़ी हुई और समुदाय आधारित ताकतों द्वारा-जिन्हें दक्षिणपंथी जमातों की शह थी- उन्हें अपनी रचना के चलते ‘लेखक की मौत’ का जो ऐलान करना पड़ा था, वह वापस हो गया.
हांसदा सोवेंद्र शेखर- जिनके उपन्यास ‘आदिवासी विल नाॅट डान्स’ को लेकर संथालों की आहत भावनाओं की बढ़-चढ़कर की गयी बातों को अदालत ने खारिज किया; मगर ऐसी कोई हरकत जूठन को लेकर खड़े किए जा रहे विवाद को लेकर बनती दिख नहीं रही है.
लेखक समुदाय अजीब-सी खामोशी की गिरफ्त में है, मुमकिन हो उनके संगठन भी मसले की गंभीरता से वाकीफ नहीं हो सके हों. अधिक चिंताजनक बात यह है कि जिस तरह एके रामानुजन को लेकर खड़े किए गए विवाद के वक्त खुद रामानुजन इस दुनिया में नहीं थे- ताकि वह अपने आलेख की हिमायत में कुछ बोल सके- वही हाल ‘जूठन’ को लेकर है.
विडंबना ही है कि एक ऐसी रचना- जिसने उत्तर भारत में 90 के दशक में उठी दलित उभार की परिघटना में नया आयाम जोड़ा था और शेष समाज के संवेदनशील तबके को झकझोर कर रख दिया था तथा आत्मपरीक्षण के लिए प्रेरित किया था – उससे ‘आहत’ लोगों को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए खुद वाल्मीकि भी दुनिया में नहीं हैं.
याद कर सकते हैं 1997 में आयी आत्मकथा ‘जूठन’ आते ही चर्चित हुई थी. उस वक्त एक सीमित दायरे में ही उसके लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि का नाम जाना जाता था. मगर हिन्दी जगत में किताब का जो रिस्पॉन्स था, जिस तरह अन्य भाषाओं में उसके अनुवाद होने लगे, उससे यह नाम दूर तक पहुंचने में अधिक वक्त नहीं लगा.
यह अकारण नहीं था कि इक्कीसवीं सदी की पहली दहाई के मध्य में वह किताब अंग्रेजी में अनूदित होकर कनाडा तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गयी थी.
उपरोक्त आत्मकथा ‘जूठन’ का वह प्रसंग शायद ही कोई भूला होगा, जब इलाके के वर्चस्वशाली जाति से जुड़े किसी सुखदेव के घर हो रही अपनी बेटी की शादी के वक्त अपमानित की गयी उस नन्हे बालक (स्वयं ओमप्रकाशजी) एवं उसकी छोटी बहन माया की मां ‘उस रात गोया दुर्गा’ बनी थी और उसने त्यागी को ललकारा था और एक ‘शेरनी’ की तरह वहां से अपनी संतानों के साथ निकल गयी थी.
कल्पना ही की जा सकती है कि जिला मुज़फ़्फ़रनगर के एक गांव में, जो 21 वीं सदी की दूसरी दहाई में भी वर्चस्वशाली जातियों की दबंगई और खाप पंचायतों की मनमानी के लिए कुख्यात है, आज से लगभग साठ साल पहले इस बगावत क्या निहितार्थ रहे होंगे. उनकी मां कभी उस शख्स के दरवाजे नहीं गयी.
इस नन्हे बालक के मन पर अपनी अनपढ़ मां की यह बगावत, जो वर्णसमाज के मानवद्रोही निजाम के तहत सफाई के पेशे में मुब्तिला थी और उस पेशे की वजह से ही लांछन का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी, गोया अंकित हो गयी, जिसने उसे एक तरह से तमाम बाधाओं को दूर करने का हौसला दिया.

प्रश्न उठता है कि ‘बस्स! बहुत हो चुका’ जैसा कविता संग्रह हो या ‘सलाम’ शीर्षक से आया कहानी संग्रह हो या ‘दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र’ जैसी रचना हो या ‘सदियों का सन्ताप’ जैसी अन्य पुस्तक हो, साहित्य के इन तमाम रूपों के जरिए एक विशाल तबके के लिए अपमान-जिल्लत भरी जिंदगी जीने की मजबूरी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखनेवाले ओमप्रकाश वाल्मीकि की सबसे चर्चित रचना को अचानक निशाना बनाने की वजह क्या है?
ऐसी परिस्थिति आज नहीं तो कल विकसित होगी इसकी भविष्यवाणी गोया वाल्मीकिजी ने अपनी रचना में की थी? अपनी कविता ‘उन्हें डर है’ में उन्होंने साफ लिखा था:
उन्हें डर है
बंजड़ धरती का सीना चीर कर/अन्न उगा देने वाले सांवले खुरदरे हाथ
उतनी ही दक्षता से जुट जायेंगे /वर्जित क्षेत्र में भी
जहां अभी तक लगा था उनके लिए / नो एंटरी का बोर्ड..… उन्हें डर है
भविष्य के गर्भ से चीख-चीखकर/बाहर आती हजारों साल की वीभत्सता
जिसे रचा था उनके पुरखों ने भविष्य निधि की तरह/कहीं उन्हें ही न ले डूबे किसी अंधेरी खाई में
जहां से बाहर आने के तमाम रास्ते/स्वयं ही बंद कर आये थे
सुग्रीव की तरह
‘जूठन’ को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए जाने की इस मांग को कैसे समझा जाए, यह मसला विचारणीय है.
क्या यह कहा जाना मुनासिब है कि समाज एवं साहित्यजगत पर हावी ऐसे लोग अभी भी उस सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते कि भारत में जातिप्रथा सदियों से उपस्थित रही है, जिसने शुद्धता और छूआछूत के नाम पर समाज के बड़े हिस्से को बुनियादी मानव अधिकारों से भी वंचित रखा है और आधुनिकता के आगमन के बाद ही इस संरचना में पहली बार कुछ हरकत, बदलाव की गुंजाइश दिख रही है?
अपनी चर्चित रचना ‘अछूत कौन और कैसे?’ जिसमें वह अस्पृश्यता के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, डॉ. आंबेडकर ने इसी दोहरे रूख की पड़ताल की थी.
सनातन धर्मांध हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई दोष है. उसके लिए यह सामान्य स्वाभाविक बात है. वह इसके लिए किसी प्रकार के पश्चात्ताप और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता.
आधुनिक हिंदू छुआछूत को कलंक तो समझता है लेकिन सबके सामने चर्चा करने से उसे लज्जा आती है. शायद इससे कि हिंदू सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण एवं कलंकित प्रणाली या संहिता है जिसकी साक्षी छूआछूत है.
डॉ. आंबेडकर, अछूत कौन और कैसे?
विडंबना ही है कि जाति प्रथा के महज उल्लेख से-उसके वर्णन से- भावनाएं आहत होने के मामले में हिमाचल प्रदेश के भद्रजन अकेले नहीं कहे जा सकते.
अभी कुछ समय पहले उधर मलेशिया में भारतीय मूल के निवासियों की गिरफ्तारी का मसला अचानक सुर्खियां बना था. बताया गया था कि ‘हिन्ड्राफ’ (Hindraf) नामक संगठन के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि मलेशिया के स्कूलों में बच्चों के अध्ययन के लिए जो उपन्यास लगाया गया था, वह कथित तौर पर भारत की ‘छवि खराब’ करता है.
आखिर उपरोक्त उपन्यास में ऐसी क्या बात लिखी गयी थी, जिससे वहां स्थित भारतवंशी मूल के लोग अपनी ‘मातृभूमि’ की बदनामी के बारे में चिंतित हो उठे थे.
अगर हम बारीकी से देखें तो इस उपन्यास में एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो तमिलनाडु से मलेशिया में किस्मत आजमाने आया है और वह यह देख कर हैरान होता है कि अपनी मातृभूमि पर उसका जिन जातीय अत्याचारों से साबका पड़ता था, उसका नामोनिशान यहां नहीं है.
यह सवाल किसी ने नहीं उठाया कि अपने यहां जिसे परंपरा के नाम पर महिमा-मंडित करने में हम संकोच नहीं करते हैं, उच्च-नीच अनुक्रम पर टिकी इस प्रणाली को मिली दैवी स्वीकृति की बात करते हैं, आज भी आबादी के बड़े हिस्से के साथ (जानकारों के मुताबिक) 164 अलग-अलग ढंग से छूआछूत बरतते हैं, वही बात अगर सरहद पार की किताब में उपन्यास में ही लिखी गयी तो वह उन्हें अपमान क्यों मालूम पड़ती है.
और मलेशिया में बसे अप्रवासी भारतीय अनोखे नहीं है.
अमेरिका की सिलिकॉन वैली- सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस इलाके में दुनिया के सर्वाधिक बड़े टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के दफ्तर हैं- में तो कई भारतवंशियों ने अपनी मेधा से काफी नाम कमाया है. मगर जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना होने लगी, तब हिंदू धर्म के बारे में एक ऐसी आदर्शीकृत छवि किताबों में पेश की गयी, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था.
अगर इन किताबों को पढ़कर कोई भारत आता तो उसके लिए न जाति-अत्याचार कोई मायने रखता था, न स्त्रियों के साथ दोयम व्यवहार कोई मायने रखता था. जाहिर है हिंदू धर्म की ऐसी आदर्शीकृत छवि पेश करने में रूढ़िवादी किस्म की मानसिकता के लोगों का हाथ था, जिन्हें इसके वर्णनमात्रा से भारत की बदनामी होने का डर सता रहा था.
साफ था इनमें से अधिकतर ऊंची कही जानेवाली जातियों में जन्मे थे. अंततः वहां सक्रिय सेकुलर हिंदुस्तानियों को, आंबेडकरवादी समूहों तथा अन्य मानवाधिकार समूहों के साथ मिल कर संघर्ष करना पड़ा और तभी पाठ्यक्रमों में उचित परिवर्तन मुमकिन हो सका.
यह दलील दी जा रही थी कि हिंदूओं में जाति एवं पुरुष सत्ता का चित्रण किया जाएगा तो वह ‘हिंदू बच्चों को हीन भावना’ से ग्रसित कर देगा और उनकी ‘प्रताड़ना’ का सबब बनेगा, लिहाजा उस उल्लेख को टाला जाए.
ऊपरी तौर पर आकर्षक लगनेवाली यह दलील दरअसल सच्चाई पर परदा डालने जैसी है क्योंकि वही तर्क फिर नस्लवाद के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किताबों से उसकी चर्चा को गायब किया जा सकता है.
वैसे दलित लेखन को लेकर कथित वर्चस्वशाली जातियों की प्रतिक्रिया बरबस अश्वेत लेखन को लेकर श्वेत प्रतिक्रिया की याद ताजा करती है:
किसे गुणवत्तापूर्ण (श्वेत) साहित्य कहा जाए इसे लेकर उच्च नीचअनुक्रम (हाईरार्की) की दुराग्रही अवधारणा और फिर उसी साहित्य में किन (श्वेत) पात्रों को मानवीय समझा जाए और उनकी जिंदगियों की नकारात्मक घटनाओं को लेकर एक विमर्श बना है.
यह कोई बौद्धिक या आकलन का मुददा नहीं है; यह नस्लीय मुददा है…
… महान अश्वेत लेखक जेम्स बाल्डविन ने लिखा है कि किस तरह श्वेतजन अपने खुद के अस्तित्व को लेकर उन भ्रांतियों -भ्रमों (जिन्हें श्वेत वर्चस्व ने गढ़ा है) से रूबरू होने से इनकार करते हैं, जिनको वह निर्मित करते हैं तथा उसी पर जिंदगी गुजार देते है; किस तरह उन छद्मों से परे अपने अस्तित्व की पड़ताल करना भी उनके लिए कठिन होता है…
अंत में जब जूठन कुछ साल से पढ़ायी जा रही थी तब भावनाओं के अचानक आहत होने की बात कहां से पैदा हुई. क्या इसका ताल्लुक राज्य में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है?
साफ है कि जिस किस्म का सियासी समाजी माहौल बन रहा है, जहां मनु और उसके विचारों की हिमायत करने पर इन दिनों किसी को एतराज होना तो दूर, आप सम्मानित भी हो सकते हैं.
उस पृष्ठभूमि में डॉ. आंबेडकर के विचारों के रैडिकल अंतर्य/अंतर्वस्तु को लोगों तक पहुंचाती दिखती किताब-भले ही वह आत्मकथा हो-उस पर इन यथास्थितिवादियों की टेढ़ी निगाह जाना आश्चर्यजनक नहीं लगता.
लेखन किस तरह समूचे जनसमूह को आंदोलित करता है फिर वह साहित्यिक लेखन क्यों न हो, इसे इतिहास की तमाम घटनाओं से समझा जा सकता है. हम याद कर सकते हैं कि ‘अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन- जिन्होंने गुलामी की प्रथा की समाप्ति के लिए जंग लड़ी थी- ने एक उपन्यास की लेखिका हैरिअट बीचर स्टो से पहली बार मिल कर क्या कहा था? (1862)
मालूम हो कि स्टो का उपन्यास ‘अंकल टाॅम्स केबिन’ जिसका फोकस दासता विरोधी था, की तीन माह के अंदर तीन लाख से अधिक प्रतियां बिकी थीं, जिसे यह श्रेय दिया जाता है कि उसने अमेरिकी प्रबुद्ध समाज के एक हिस्से में दासप्रथा के विरोध में माहौल बनाया था.
लिंकन ने कहा था कि ‘तो यह हैं वह छोटी मोहतरमा/स्त्री जिसने इस बड़े युद्ध की चिंगारी फेंकी थीं’ (So this is the little lady who made this big war.)
उत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि पचास-साठ के दशकों में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललई सिंह यादव ‘पेरियार’, रामस्वरूप वर्मा आदि कइयों ने अपने लेखन से जो अलख जगाए रखी, अपने सामाजिक सांस्कृतिक प्रबोधन से उत्पीड़ित समुदाय को मुक्ति के फलसफे से अवगत कराया, भाग्यवाद के घटिया चिंतन से तौबा करना सिखाया, उसी मुहिम ने तो बाद में दलित-उत्पीड़ित दावेदारी की जमीन तैयार की.
इसमें कोई दोराय नहीं कि पचास-साठ के दशकों से हालात काफी बदले हैं, मगर इसके बावजूद ऐसे विचारों की ताप समाप्त नहीं हुई है. वह नए नए नौजवानों को आमूल-चूल बदलाव के फलसफे से रूबरू करा रही है.
ऐसे उथलपुथल भरे माहौल में भारतीय समाज की तीखी आलोचना करनेवाली एक बेहद लोकप्रिय रचना निहित स्वार्थी तत्वों को कैसे बर्दाश्त हो सकती है, जो न केवल यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं बल्कि वह अपने अतीत के महिमामण्डन में ही मुब्तिला रहते हैं.
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक हैं.)