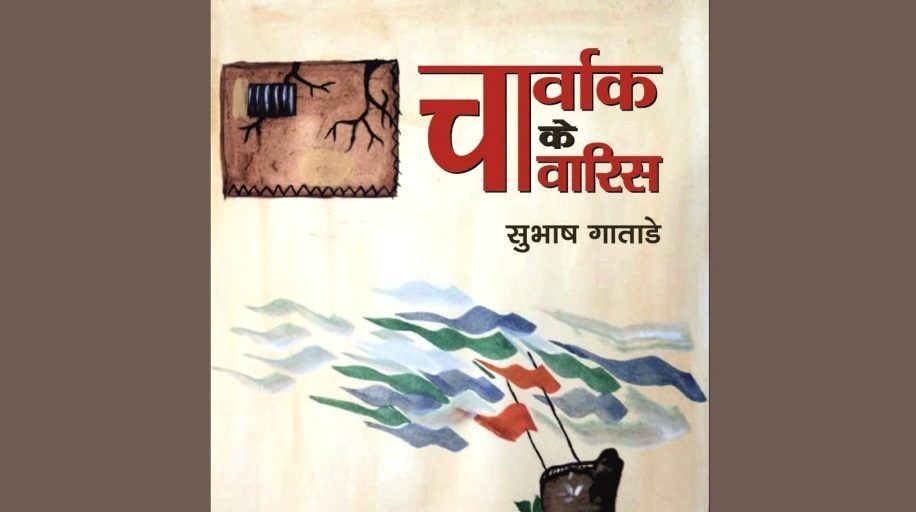यह निबंध-संग्रह ‘एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति’ के स्वनामधन्य पैरोकारों की असली-नकली अवधारणाओं और कुतर्कों की बिना पर रचे जा रहे तिलिस्म को वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया की कसौटी पर कसकर न सिर्फ बेपरदा बल्कि पूरी तरह ख़ारिज भी करता है.

कोई दो राय नहीं कि इन दिनों हमारा देश ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिशों की बात पुरानी पड़ गई है और विचारों को ही द्रोह साबित किया जा रहा है.
इतना ही नहीं, ऐसा साबित करने में लगी जमातों ने विचारों और विचारकों पर जो युद्ध जानबूझकर थोप दिया है, उसे वे स्पेक्ट्रम की तरह पसराती जा रही हैं. अलबत्ता, इस सिलसिले में अच्छी बात यह है कि इन जमातों के मंसूबों के बिल्कुल विपरीत उनका प्रतिरोध चुकने या रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है.
इसी प्रतिरोध की एक कड़ी जन सरोकारों से प्रतिबद्ध लेखक सुभाष गाताड़े द्वारा लिखे और स्वदेश कुमार सिन्हा द्वारा संपादित निबंधों का हाल ही में प्रकाशित संग्रह ‘चार्वाक के वारिस’ भी है. इसके निबंधों को पढ़ते हुए लगातार लगता है कि इनका लेखक हर हाल में इस ‘द्रोह’ पर ‘आमादा’ है.
वैसे भी देश में जो लोग खुद को चार्वाक की विद्रोही परंपरा का वारिस मानते हैं, वर्तमान हालात में उनके लिए इस प्रतिरोध से विरत रहना मुमकिन नहीं है.
इस बात को संग्रह की इस केंद्रीय चिंता से समझा जा सकता है कि ‘हर वो स्थान, हर वह माध्यम, जो विचारों के मुक्त प्रवाह को सुगम बना दे, मनुष्य के दिमाग को ‘तर्क करने के साहस’ के लिए प्रेरित कर सके, उसे बाधित करने के लिए-फिर वह चाहे शिक्षा संस्थान हों, पाठ्य पुस्तकें/किताबें हों या सार्वजनिक दायरे में व्याप्त खुलापन हो- राज्य सत्ता के इदारे ही नहीं, ऐसी जमातें भी सक्रिय हैं, जो ‘एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति’ के प्रसार के उद्देश्य के तहत आगे बढ़ रही हैं.’
सच पूछिए तो वे इन जमातों की ही कारस्तानियां हैं, जिनके चलते आज ‘सार्वजनिक विमर्श उस विडंबनापूर्ण स्थिति में जा पहुंचा है कि असली लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं और छद्म नामों से जितना भी जहर उगला जा सके, उस पर कोई रोक नहीं है. अपने देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में खास समुदायों को निशाना बनाकर महज फर्जी खबरों के सहारे चंद लम्हों में आग लगाई जा सकती है.’
प्रसंगवश, भले ही भारत के संविधान की धारा 51-ए कहती हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना और वैज्ञानिक व तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना देश के हर नागरिक और साथ ही राज्य का कर्तव्य है, हिन्दी के लेखकों-साहित्यकारों के कई हिस्सों में ऐसी चिंताओं को केंद्र में रखने को कौन कहे, चिंताओं की तरह लेने या चिंताएं मानने का ही रिवाज नहीं है.
उल्टे कई मायनों में उन्हें मजे के लिए इस्तेमाल कर विमर्श का ढोंग रचा जाता और ‘एंजॉय’ किया जाता है. कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे में यह निबंध-संग्रह अकाल के फल जैसा तो है ही, एक बड़े अभाव की पूर्ति भी करता है.
सबसे ज्यादा इस अर्थ में कि यह ‘एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति’ के स्वनामधन्य पैरोकारों द्वारा अनेक असली-नकली अवधारणाओं, मिथकों, इतिहासों और कुतर्कों वगैरह की बिना पर षडयंत्रपूर्वक रचे जा रहे तिलिस्म को वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया की कसौटी पर कसकर न सिर्फ बेपरदा या तार-तार बल्कि पूरी तरह निरस्त्र भी करता है.
इसमें लेखक पूरी शिद्दत से इस गंभीर सवाल का उत्तर भी तलाश करता है कि देश में अतार्किक, असमावेशी, असहिष्णु एवं असमानतामूलक राजनीति का दबदबा सिर्फ दक्षिणपंथ की सफलता का नतीजा है या ऐसे रूपांतरण की जड़ें भारतीय समाज व संस्कृति में पहले से मौजूद रही हैं?
उसका उत्तर कुछ लोगों को थोड़ा अप्रिय, असुविधाजनक या झुंझलाहट पैदा करने वाला लग सकता है, लेकिन इन लोगों की बेचारगी यह कि अपने उत्तर को उसकी परिणति तक ले जाने के क्रम में लेखक तार्किकता के ऐसे कवच से लैस नजर आता है कि संग्रह के ‘थोड़ा-सा विज्ञान और थोड़ी-सी माया’ शीर्षक निबंध में उल्लिखित पोंगापंथियों का यह कुतर्क भी उस पर असर नहीं करता कि ‘तर्क-वितर्क द्वारा तत्वज्ञान होना असंभव है.’
और ‘तर्क की सार्थकता सिर्फ इतनी है कि उसका उपयोग धर्मशास्त्रों में लिखी गई बातों को सत्य सिद्ध करने के लिए किया जाये.’
अच्छी बात यह है कि संग्रह में लेखक न कोई छद्म रचता है, न ही कोई खोल ओढ़ता है. उसने एकदम बेलौस होकर इसको ‘समाज, संस्कृति और सियासत पर एक प्रश्नवाचक’ करार देते हुए भारत के समाज, संस्कृति और सियासत से रूबरू होने की कोशिश बताया है.
अपने सरोकारों पर प्रकाश डालते हुए उसने लिखा है कि ‘विचार जब जनसमुदाय द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, तब वह एक भौतिक शक्ति बन जाते हैं. कितनी दुरुस्त बात कही थी कार्ल मार्क्स ने. अलबत्ता यह स्थिति बिल्कुल विपरीत अंदाज में हमारे सामने नमूदार हो रही है. जनसमुदाय उद्वेलित भी है, एक भौतिक ताकत के रूप में उपस्थित भी है, फर्क बस इतना ही है कि उसके जेहन में मानवमुक्ति का फलसफा नहीं, बल्कि ‘हम’ और ‘वे’ की वह सियासत है जिसमें धर्मसत्ता, पूंजीसत्ता और राज्यसत्ता के अपवित्र कहे जा सकने वाले गठबंधन के लिए लाल कालीन बिछी है.’
लेखक इसे लेकर किसी दुविधा में नहीं है कि इस लाल कालीन को बटोरना और विचारों को नए सिरे व नई अंतर्वस्तु के साथ भौतिक ताकत बनाना है ताकि मानवमुक्ति की बातें एजेंडे पर आएं तो उसके लिए हर एक को बकौल युवा मार्क्स ‘महान ऊंचा लक्ष्य’ तय करना होगा और उसके लिए चुनना होगा ‘उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम’ ताकि ‘आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान’ में ‘असली इंसान की तरह’ जिया जा सके.
क्रांतिज्योति सावित्री बाई फुले और उनकी अनन्य, फिर भी विस्मृत कर दी गई, सहयोगी सुश्री फातिमा शेख को समर्पित यह निबंध संग्रह चार खंडों में विभाजित है. पहले भाग में देश व समाज के तमाम अटपटे कार्य-व्यवहारों, विसंगतियों व विडंबनाओं की राहुल सांकृत्यायन जैसे चिंतकों के नजरिये से पड़ताल की गई है.
जैसा कि विदित है, राहुल सांकृत्यायन मानते रहे हैं कि ‘मानसिक दासता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है’ और ‘जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दासता के बंधन उतने ही अधिक होते हैं. भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं और इसीलिए उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं.’
चूंकि सुभाष वामपंथ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पड़तालों की अंतर्वस्तु अपने मूल रूप में मार्क्सवादी है. लेखकीय विनम्रतावश, संग्रह के फोकस को ‘बहुत सीमित’ बताते हुए वे लिखते हैं, ‘मार्क्स से आप सहमत-असहमत हो सकते हैं. मगर हमारे वक्त में वह इस वजह से और भी मौजूं दिखते हैं कि अपने विचारों के बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहने और उनके लिए संघर्ष करते रहने की बेहद शानदार नजीर पेश करते हैं.’

हां, जैसा कि संग्रह के नाम से भी जाहिर है, सुभाष अपने विश्लेषणों को देश के ‘बार्हस्पत्य’ नाम से जाने-जाने वाले प्रसिद्ध अनीश्वरवादी भौतिकवादी विद्वान चार्वाक की उस विद्रोही परंपरा से जोड़ते और उसकी विरासत को समृद्ध करने पर जोर देते हैं.
उसके द्वारा पारलौकिक सत्ताओं को अस्वीकार करने के विरुद्ध खुन्नस निकालने के लिए इन सत्ताओं के समर्थकों ने कभी जिसके सिद्धांत व दर्शन को वेदवाह्य करार दिया और कभी अपनी हिकारत की सारी निगाहें उसके नाम कर दीं.
संग्रह के दूसरे भाग में देश की जाति समस्या तथा उसके उन्मूलन के रास्ते की चुनौतियों की चर्चा की गई है, तो तीसरे में बहुसंख्यकवाद की चुनौतियों की, जबकि चौथे में महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा व अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर की हिन्दी में प्रकाशित तीन जरूरी किताबों की समीक्षा की गई है.
संग्रह का वह ‘परिशिष्ट’ भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें सात अपनी तरह के अनूठे उल्लेख हैं. संग्रह के निबंधों पर अलग-अलग और विस्तार से चर्चा का अवकाश यहां नहीं है, लेकिन संक्षेप में कहना होगा कि उनके विषयों में खासा वैविध्य है.
वे हमारे राजनीतिक से लेकर सामाजिक, आार्थिक व सांस्कृतिक ढांचों व उनके अच्छे-बुरे प्रवाहों की ऐसी सूक्ष्मदर्शी विवेचना करते हैं कि सुभाष द्वारा अपने अभिन्न मित्र आनंद तेलतुम्बड़े के बारे में कही हुई यह बात खुुद उन पर भी लागू की जा सकती है.
आनंद के बारे में वे लिखते हैं कि ‘मुझे हमेशा ताज्जुब हुआ है कि आनंद इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? आनंद की हर किताब अपनी अंतर्वस्तु में मौलिक रही है और अलग-अलग मसलों पर प्रकाशित उनके लेखों में भी हम एक मौलिकता देखते आये हैं. उन्होंने हर मसले को, हर समस्या को हमेशा गैर पारंपरिक तरीके से संबोधित करने की कोशिश की है.’
निस्संदेह ‘चार्वाक के वारिस’ में सुभाष के साथ भी कुछ ऐसा ही है. हां, यहां आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर राम पुनियानी याद आते हैं, जिन्होंने दिसंबर, 2004 में देश में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए पूर्णकालिक कार्य करने की इच्छा के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और तभी से सुभाष की ही तरह पहल करते हुए उन मिथकों के तार्किक खंडन में लगे हुए हैं, जिन पर सांप्रदायिक कट्टरवाद अपने साजिशी दुष्प्रचारों का तकिया रखता रहा है.
अगर देश को इस कट्टरवाद की साजिशों के पार जाना है, गोयाकि पार गये बिना उसका निस्तार नहीं है, तो यकीनन, उसे ऐसे और सुभाष गाताड़े और राम पुनियानी पैदा करने होंगे. जैसा कि शुरू में कह आये हैं कि इस वक्त जब इस देश में विचारों को ही द्रोह साबित किया जा रहा है, चार्वाक के वारिसों के लिए यह ‘द्रोह’ समय की मांग हो गया है.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)