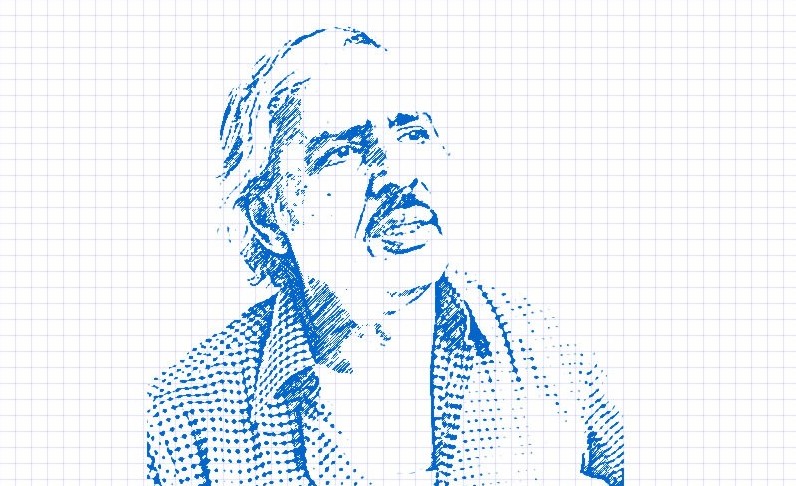स्मृति शेष: सागर सरहदी इस एहसास के साथ जीने की कोशिश करते रहे कि दुनिया को बेहतर बनाना है. मगर अपनी बदनसीबी के सोग में इस द्वंद्व से निकल ही नहीं पाए कि साहित्य और फिल्मों के साथ निजी जीवन में भी एक समय के बाद अपनी याददाश्त को झटककर ख़ुद से नया रिश्ता जोड़ना पड़ता है.
![सागर सरहदी [जन्म: 1933-अवसान 2021] (फोटो साभार: ट्विटर/@SagarSarhadi)](https://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/04/Sagar-Sarhadi-Photo-Twitter-acc.jpg)
ये विभाजन की त्रासदी और विस्थापन का ऐसा कटु अनुभव है जिसके घटनाक्रम, काल और किरदार; हमारी सियासत के हाथों अर्थहीन होकर हर दूसरे दिन इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं. तो क्या दो हज़ार इक्कीस भी सन सैंतालिस के सोग में है?
‘सब मर गए, सब डूब गए और मैं बच गया…अपनी यादों के भूत लिए…’
वो 1947 का ज़माना था. सागर अपने जिस्म का बोझ उठाए निढाल चले जा रहे थे. गांव, घर और बहता दरिया सब कहीं पीछे अतीत के गर्भ में समा रहे थे. अंतहीन ख़ालीपन से अटे हुए क़दम प्यास की शिद्दत में टूट रहे थे.
ऐसे में किसी फ़रिश्ते की तरह पानी का प्याला लिए, उनके क़रीब आती हुई लड़की अचानक अपनी सहेलियों की तरफ़ मुड़ी और चीख़ पड़ी;
‘हिंदू है…’
उसी लम्हे ‘मज़हब’ के हाथों इंसानियत का क़त्ल हो गया… ये चीख़ जीवन भर सागर सरहदी का कलेजा नोचती रही. उनको अपने नाम से नफ़रत हो गई. अरसे बाद उन्होंने इस दर्द को पूरी शिद्दत से लिखा और उस पर कई बार अपने दस्तख़त किए;
‘मैं अपनी शनाख़्त खो बैठा हूं. एक कॉम्प्लेक्स लिए घूमता हूं कि मैं इंसान नहीं हिंदू हूं…’
सियासी हंगामे में सिर्फ़ हिंदू हो जाने का दर्द सागर को सालता रहा, और जब उन्होंने ‘मिर्ज़ा साहिबां’ नाटक लिखा तो उसमें भी वो प्यास की इसी शिद्दत में जलते नज़र आए.
शायद ये दूसरी कर्बला थी, जो उनकी ज़बान पर छाले की तरह बैठ गई;
‘मलिक: मैंने कहा. मैं राम का नाम रसूल रख दूंगा तो क्या राम का नाम बदल जाएगा? उसकी शक्ल बदल जाएगी? उन्होंने जवाब दिया ‘उसकी रूह बदल जाएगी.’
साहिबां; फिर?
मलिक: मैंने कहा रूह किसने देखी है? उन्होंने जवाब दिया. ‘हिंदू रूह होती है. मुसलमान रूह होती. जैसे हिंदू पानी होता है मुसलमान पानी होता है…’
मैं यहां डासना का ज़िक्र नहीं करना चाहता, बस बड़बड़ाना चाहता हूं कि राम का नाम रसूल या रसूल का नाम राम रखने की इंसानियत धर्म के पास शायद कभी नहीं थी.
ये क़िस्सा पानी का नहीं इंसानियत के मर जाने का है.
बहरहाल सागर सरहदी को याद करते हुए मुझे कुछ और कहना था और शायद आपको भी ये सब नहीं सुनना था, लेकिन क्या कीजिए कि किसी रचनाकार से उस वक़्त तक साक्षात्कार मुमकिन नहीं जब तक कि उसके बुनियादी तजरबे को कुरेद न लिया जाए.
हां, सागर का बुनियादी तजरबा हिजरत और विस्थापन का था, जो बाद में उनके यहां एक तरह के विषाद और अवसाद से लड़ने और उससे रिहाई पाने की सूरत में भी हमेशा शोर मचाता रहा.
दरअसल वो इस एहसास के साथ जीने की कोशिश करते रहे कि दुनिया को बेहतर बनाना है. मगर अपनी बदनसीबी के सोग में इस द्वंद्व से निकल ही नहीं पाए कि साहित्य और फिल्मों में एक समय के बाद बल्कि निजी जीवन में भी अपनी याददाश्त को झटककर अपने आपसे नया रिश्ता जोड़ना पड़ता है.
बदनसीबी ही कह लीजिए कि उनके यहां ऐसा नहीं हुआ, और वो अपने बुनियादी तजरबे की मिट्टी में ढलते चले गए.
हालांकि वो प्रगतिशील लेखकों की सोहबत में रहे, इप्टा के लिए नाटक लिखे, झुग्गी और बस्तियों में इंसानियत के नारे बुलंद किए. दुनिया भर के बड़े लेखकों की इंक़लाबी किताबें पढ़ते रहे, सेक्स और प्रेम की गुत्थियां सुलझाते रहे…
एक अजीब सी ‘गुमशुदगी’ उन पर तारी रही. फिर नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता ने उनको संभलने नहीं दिया. इन सबने गंगा सागर तलवार को सागर सरहदी तो बना दिया, लेकिन वो अपनी सोच के मकड़जाल में फंसे रह गए.
बस अफ़सोस कि मौजूदा पाकिस्तान के एबटाबाद बफ़ा में 11 मई 1933 को जन्मे सरहदी ने विभाजन के बाद अपनी मौत तक सिर्फ़ एक शरणार्थी का ही जीवन-बसर नहीं किया बल्कि दिल्ली और बंबई के शुरुआती दिनों में चूल्हे और चक्की की उदासी भी उन्हें तोड़ती चली गई.
कहां तो बफ़ा में बाप का रुतबा था, अपनी ठेकेदारी थी और यहां ढंग का ठिकाना तक नसीब नहीं था. एक ही कमरे में बाप, भाई, भाभी और उनके बच्चों के साथ सरहदी ज़िंदगी की तंग करवटों को पहलू बदलते देखते रहे.
उजड़ जाने का एहसास ऐसा था कि विवाह जैसी संस्था से ही मुंह फेर लिया. बाद में ये भी मानने लगे कि शादी के बाद पढ़ना-लिखना नहीं हो पाता.
ये और बात है कि उनके बेहद क़रीबी रहे चर्चित कथाकार सलाम बिन रज्ज़ाक़ की गवाही कहती है कि उनको पढ़ने से ज़्यादा किताबें ख़रीदने का शौक़ था. हर बंधन और क़ैद से रिहाई की ख़्वाहिश ने उन्हें किताबें दीं, वो दिल्ली और बंबई में जैसे-तैसे पढ़-लिख भी गए. लेकिन अंततः अपने एकांत की भट्टी में जल बुझ गए.
इस जल बुझ जाने के अमल में उन्होंने कई औरतों (उनके शब्दों में दर्जन भर से ज़्यादा) से ‘प्रेम’ किया और हर बार यही कहते रहे कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा. उनको शादी करनी थी…
हां, उन्होंने औरतों से अपनी हमदर्दी का इज़हार किया, उनकी आज़ादी की बात भी की और इस मुल्क को उनके लिए ‘क़त्लगाह’ तक कहा… मगर जब लिखने का समय आया तो अपने आप से पूछने लगे कि औरत की आंखों से किस हद तक रोमांस किया जा सकता है?
एक बार ऐसा भी हुआ कि वो पार्टी के बीच से ये सोचकर रोते हुए भाग निकले कि एक शरणार्थी जो मार्क्सवाद में यक़ीन रखता है, वो शराब और शबाब में क्या तलाश कर रहा है? मुझे तो इंक़लाब लिखना है…
हालांकि उनके यहां रोमांस और इंक़लाब के बीच औरत सिर्फ़ स्लीपिंग पार्टनर है…
अब उनकी फिल्म ‘बाज़ार’ कुछ पाकिस्तानी आलोचकों के अनुसार ‘इस्लामी फिल्म’; को चाहें तो आप कालजयी समझें, क्लासिक का दर्जा दें या इंक़लाब कह लें. मुझे बस ये कहना है कि उनके आदर्शों की औरत उनकी रचनाओं में उनके ‘ऑल्टर ईगो’ [ Alter Ego] का शिकार है.
ये संयोग नहीं कि वो अपनी रचनाओं में सबसे ज़्यादा औरत और मर्द के रिश्तों पर बात करते हैं, और अक्सर अपनी आत्ममुग्धता में सेक्स को प्रेम का नाम ही नहीं देते बल्कि मर्द के अहम् के सामने औरत को हेच भी बता देते हैं;
‘जब कोई लड़की मुझसे वास्ता रखना चाहती है तो सबसे पहला ख़याल जो मेरे दिमाग़ में आता है ये होता है कि वो मेरे साथ सोए…’
‘हिंदुस्तानी औरत की झिझक उसमें नहीं थी. चाहती तो ख़ुश करने में कोई कसर न उठा रखती थी. सेक्स के बारे में जितना मैंने पढ़ा था, गीता के जिस्म ने सब भुला दिया था.’
‘औरत बच्चों के बिना कभी मुकम्मल औरत नहीं बन सकती.’
ये उनकी कुछ कहानियों के ओझल हिस्से हैं. इससे अलग अगर फिल्म ‘बाज़ार’ की नजमा (स्मिता पाटिल) का एक संवाद याद करें जो वो लेखक सलीम (नसीरुद्दीन शाह) से कहती है कि; ‘शादी के बारे में रावी इंतिज़ार लिखता है’ तो महसूस होगा कि नजमा दरअसल सागर ख़ुद हैं.
मैं यहां अलग से सागर के प्रेम, रोमांस और सेक्स के दायरे में फंसी औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता. लेकिन यक़ीन दिलाता हूं कि अगर यश चोपड़ा की कभी कभी, सिलसिला, और चांदनी जैसी फिल्में न होतीं तो वो औरत की आंखों का रोमांस भी न लिख पाते.
सागर कई मानों में उर्दू की दक़ियानूसी किताबों की तरह सोचते थे, या यूं कह लें कि उनका हमज़ाद (Alter Ego) उनके आदर्शवाद को क़ायम नहीं रहने देता है.
फिल्म ‘बाज़ार’ के बनने का ही क़िस्सा याद करें तो वो संसाधन न होने के बावजूद यश चोपड़ा की मदद (उनके शब्दों में दख़लअंदाज़ी) को ठुकराकर अपनी तरह का सिनेमा बनाने की ज़िद पालते हैं.
एक लेखक की ज़िद को किसी हद तक ये फिल्म साकार भी करती है. शायद इस बात की भी दाद उनको मिलनी चाहिए कि वो इप्टा के दोस्तों की आलोचना के बावजूद अपने यक़ीन को अमली जामा पहनाते हैं. लेकिन क्या ‘सब्जेक्ट’ के अलावा इस फिल्म में ‘सिनेमा’ है?
कहानी की कमियों और उर्दू कहानी की शुरुआती परंपरा की पैरवी को नज़रअंदाज़ भी कर दें, तो इसका स्क्रीनप्ले और कैमरे की समझ निम्नस्तरीय है.
ये ठीक है कि वो पहली बार सिनेमा में सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे और अपने सब्जेक्ट के सामने तमाम दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता भी नहीं दे रहे थे तो भी हद से ज़्यादा लाउड डायलॉग और किताबी भाषा हमें एक अच्छे सिनेमा से वंचित कर देती है?

ये और बात है कि ‘बाज़ार’ के नग़्मे और ख़य्याम की मौसीक़ी हमें इस एहसास से दो-चार नहीं होने देते. इसके बावजूद मैं ‘बाज़ार’ को एक ज़रूरी सिनेमा मानता हूं. इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो फुल लेंथ सिनेमा नहीं लिख सकते थे, अलबत्ता ये ज़रूर समझता हूं कि सागर किसी हद तक पटकथा और संवाद लेखन में ही अपना बेहतरीन दे सकते थे जो उन्होंने कई फिल्मों में दिया भी.
मैंने अभी उर्दू की दक़ियानूसी किताबों वाली बात कही तो ‘बाज़ार’ में शबनम (सुप्रिया पाठक) का ज़हर खा लेना और नजमा का इक़बाल-ए-जुर्म जैसा कुछ उस लेखक का ढोंग बन गया है जो ख़ुद को मार्क्सिस्ट कहता है.
दरअसल हर बार उनका ऑल्टर ईगो उनको फरार की राह दिखा देता है,‘बाज़ार’ में भी लेखक के तौर पर मौजूद सलीम का ये कहना कि ‘मैं इस ख़राबे की सैर कर चुका हूं बस, मैं निकल जाता हूं’… तो महसूस होता है कि वो उस औरत से रिश्ता तो रखना चाहता है जिसका प्रेमी पहले से है, बस वो ये कहना नहीं जानता कि; ‘उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे…’
संयोग देखिए कि;
‘अगर कहीं मुलाक़ात हो गई तो पहचान लोगी मुझे.
सलाम ज़रूर करूंगी.’ (फिल्म: बाज़ार)
‘आदमी: अगर आप मुझे कहीं, किसी जगह पर दोबारा मिल जाएंगी तो पहचान लेंगीं?
लड़की: आप भी कमाल की बात करते हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर यूं आपको नमस्ते कहेंगे.’ (नाटक: एक बंगला बने न्यारा)
औरत कोई भी हो, चाहे वो ‘बाज़ार’की ‘नजमा’ या ‘एक बंगला बने न्यारा’ की लड़की, सागर ये ज़रूर चाहते हैं कि वो उन्हें याद रहें. और याद रह जाने का ये मामला सागर के यहां प्रेम बिल्कुल नहीं है.
जिस ज़माने में (1982) ये फिल्म बनी उस ज़माने में समाजी सरोकार की तमाम बड़ी फिल्में बन चुकी थीं, इसके बावजूद सागर इसको उस लेखक की नज़र से नहीं लिख पाए जो मार्क्सवादी होने के साथ सिमोन द बोउआर तक के पाठक होने का दावा करता रहा.
महबूब ख़ान की ‘मदर इंडिया’ देखकर ख़ुद को शांत करने के लिए मीलों पैदल चलने वाले सागर इसमें वो नहीं दिखा पाए जिसकी बातें अक्सर करते रहे.
हां, वो हर नाइंसाफ़ी और सत्ता के दमन के ख़िलाफ़ एक लेखक की प्रतिक्रिया को ज़रूरी मानते रहे. इसलिए वो अब तक वरवरा राव जैसे समकालीन कवि और मेधा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता के क़रीबी रहे. लेकिन वो उस सोच से सीधा रिश्ता क़ायम करने में कामयाब नहीं हुए और हर बार अपने गिर्द लिपटी दुनिया को ही जाने-अनजाने सामने लाते रहे.
खैर, फिल्म और थिएटर से उनके रिश्ते की बात करें तो उनके बड़े भाई हरबंस लाल स्टेज के कलाकार थे. फिल्म डायरेक्टर रमेश तलवार उनके भतीजे हैं, जिनकी वजह से वो ‘मिर्ज़ा साहिबां’ के दौरान यश चोपड़ा के संपर्क में आए.
सागर के साथ यश चोपड़ा का नाम लाज़मी तौर पर लिया जाता है, इसलिए यहां ये याद रखना भी ज़रूरी है कि उन्होंने इससे पहले फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग की. बासु भट्टाचार्य की अनुभव उनकी पहली फिल्म थी जिसमें कपिल कुमार के साथ संवाद लेखन किया.
पिछली पंक्तियों में सलाम बिन रज्ज़ाक़ का ज़िक्र आया था तो बता दें कि कई मानों में शाहरुख़ ख़ान की पहली फिल्म ‘दीवाना’ की स्क्रिप्टसाज़ी में सागर ने सलाम से मदद ली और कई सीन भी लिखवाए. बाद में भी वो चाहते थे कि सलाम फिल्मों के लिए लिखें लेकिन उन्होंने कई वजहों से मना कर दिया.

सागर सरहदी के एक नाटक के कलाकार. (फोटो साभार: ट्विटर/@SagarSarhadi)
खैर, उनके रंगमंच पर निगाह करें तो सागर के ड्रामे स्टेज पर अक्सर फ्लॉप साबित हुए. कई बार हूटिंग का भी सामना करना पड़ा. इसी वजह से वो एक ज़माने में इप्टा से ख़फ़ा भी हुए.
बात वहीं उनके नार्सिसिज्म पर जाकर ठहरती है कि वो ड्रामे की नाकामी से ख़ुद को अलग करते हुए कहते थे;
‘जिस तरह से वो ड्रामा पेश किया गया था और जिस फॉर्मेट में डायरेक्ट हुआ था उसका फ्लॉप होना यक़ीनी था…’
अपने नाटक ‘भगत सिंह’ के फ्लॉप होने पर भी उन्होंने इसको मील का पत्थर बताते हुए कहा था कि सारा दोष डायरेक्शन का है.
बहरहाल इप्टा से उनकी नाराज़गी कैफ़ी आज़मी की वजह से दूर हुई. इस प्रसंग को बयान करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर लिखा कि, कैफ़ी साहब ने मुझसे ड्रामा लिखने को कहा जबकि उनके पास इप्टा के लिए नाटकों की कमी नहीं थी.
हां, उनके ड्रामे फ्लॉप हुए, लेकिन विषय के लिहाज़ से उनके कई नाटक महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने इंक़लाब, विभाजन और दोनों मुल्कों की सरहद को लेकर इंसानी नज़रिये को पेश किया.
हालांकि यहां भी वो औरत को अपनी मर्दवादी मानसिकता से अलग नहीं कर पाए;
‘उन्होंने (शौहर ने) मुझे ये भी बताया कि मैं शादी का बंधन तोड़ भी सकती हूं और अगर समाज से घबरा जाऊं तो शादी के लिबादे में भी पुराना रिश्ता रख सकती हूं’
‘तुम मेरे क़रीब आना शुरू कर दो. इसी तरह देखो मुझे. मेरे होंठ शहद ले आएंगे, मेरी आंखें पैमाना छलकाएंगी. आज इसी लम्हे मेरा जिस्म तुम्हारे लिए पिघलेगा.
और आज ही नहीं जब भी तुम अपनी तन्हाई का महल खड़ा करोगे, अपने दर्द की ज़बान से उसके गुंबद बनाओगे, अपनी शिकस्त का जादू जगाओगे. मेरे होंठ शहद ले आएंगे, मेरी आंखें पैमाना छलकाएंगी. मेरा जिस्म तुम्हारे लिए पिघलेगा…’
दरअसल वो ख़ुद से कभी भी वास्ता रख चुकी औरत की आज़ादी के क़ायल नहीं थे बल्कि उसके पति के ‘खुले विचारों’ का सहारा लेकर अपनी फैंटेसी को जीना चाहते थे. शायद इसलिए उनका कथित सभ्य पुरुष भी ढोंगी मालूम होता है.
अच्छी बात ये है कि उनके नाटक ‘किसी सीमा की एक मामूली-सी घटना’और ‘मसीहा’ के अक्सर एक्ट और सीन में ये महसूस होता है कि ‘रामचंद पाकिस्तानी’और ‘वॉर छोड़ न यार’ जैसी फिल्मों से बहुत पहले ऐसी कहानियां सागर स्टेज कर चुके थे.
अगर वो इस तरह के विषयों को गंभीरता से पर्दे पर पेश करने की कोशिश करते तो शायद अपनी तरह का सशक्त सिनेमा बना सकते थे.
उल्लेखनीय है कि उन्होंने ‘द कर्टेन’ नाम से अपना ड्रामा ग्रुप भी बनाया, जिसमें कई रंगकर्मियों के साथ अपने समय के बड़े आर्टिस्ट क़ादर खान ने भी ‘भूखे भजन न होय गोपाला’ में एक्ट किया.

नाटकों से अलग उनकी कहानियों के संग्रह ‘आवाज़ों का म्यूज़ियम’के अध्ययन से अंदाज़ा होता है कि वो उर्दू में औसत दर्जे की कहानियां लिख रहे थे. हालांकि उनकी दो एक कहानियों को हमारे समय में बलराज मेनरा जैसे बड़े कथाकार ने अपनी पत्रिका ‘शुऊर’ में जगह दी.
मेनरा की ही पत्रिका ‘सुर्ख़-ओ-सियाह’ के इश्तिहारी बुकलेट में उनकी कहानी ‘जीव जनावर’ को कथा साहित्य की दुनिया में ‘क़यामत’ क़रार दिया गया. जिसको शमीम हनफ़ी के शब्दों में अमानवीयता के ख़िलाफ़ सघन चीख़ भी कह सकते हैं.
याद रखने वाली बात है कि इससे पहले सागर अत्यंत सरल भाषा शैली में लिख रहे थे जबकि बाद में उन्होंने बिंब और प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक उर्दू कहानियों की तरफ़ क़दम बढ़ाया, शायद इसलिए वो मेनरा को पसंद भी आए;
‘एक ही ख़याल कोड़े बरसा रहा था,
कोई साथ,
कोई लम्स,
कोई गर्मी हो
चाहे वो औरत हो,
मर्द हो, जानवर हो…
नहीं तो भटकन होगी,
रात भर…’ (जीव जनावर)
‘जीव जनावर’ के नाम से ही बाद में उनकी कहानियों का एक संग्रह हिंदी में प्रकाशित हुआ.
उनके बारे में बात करते हुए अक्सर फिल्म और उर्दू पर भी बात की जाती है, हालांकि वो फिल्मों के लिए लफ़्ज़ ‘उर्दू’ को दुरुस्त नहीं समझते थे, उनके मुताबिक़ फिल्मों की अपनी भाषा होती है.
अंत में बस ये कि कुछ कामयाब फिल्मों की लेखनी से जुड़े रहने और ख़ुद को पेशेवर राइटर कहने के बावजूद सागर तकनीकी दुनिया से तालमेल न बिठा सके.