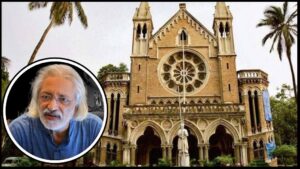हिंदी फिल्में सफलता के लिए आबादी के हर हिस्से और हर धर्म के दर्शकों पर निर्भर करती हैं. पर इस बार यहां हमारे सामने एक ऐसी फिल्म आई, जिसे सिर्फ (कट्टर) हिंदू दर्शकों की ही दरकार है.

हाल के वर्षों में हिंदी फिल्मों ने सच्चे अर्थों में भगवा झंडा फहराया है. मध्ययुगीन कथाएं, जो कि कभी-कभी कल्पना और मिथक पर आधारित होती हैं, को महाकाव्यात्मक युद्धों में तब्दील कर दिया गया है- जिनमें हिंदू राजा सिनेमाई परदे पर बर्बर और क्रूर मुस्लिम लूटेरों को पराजित करते हैं.
सद्गुणी हिंदू राजा ऊंचे कंठ से अपनी हिंदू पहचान की बार-बार घोषणा करते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे धर्मयुद्ध कर रहे हैं. यह वर्तमान सत्ता के नए अतिउग्र राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी एजेंडा से बहुत अच्छी तरह से नत्थी हो जाता है. लेकिन अब एक फिल्म वहां तक गई है, जहां तक किसी अन्य फिल्म ने कदम नहीं रखा था.
हालिया रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का एक प्रिंट विज्ञापन गर्व के साथ घोषणा करता है :‘आइए, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट का जयगान करें’. यहां किसी किस्म का संशय या भ्रम नहीं है. आज तक किसी ने भी खुलेआम तरीके से अपने संदेश को इतने साफ शब्दों में किसी एक खास समुदाय तक सीमित नहीं किया था.
वास्तविकता यह है कि हिंदी फिल्में सफलता के लिए आबादी के हर हिस्से और हर धर्म के दर्शकों पर निर्भर करती हैं. यहां हमारे सामने एक ऐसी फिल्म आई है, जिसे सिर्फ (कट्टर) हिंदू दर्शकों की ही दरकार है.

अगर आपको लगता है कि यह महज एक विज्ञापन का मामला है, तो आपको इसका ट्रेलर देखना चाहिए. माथे पर तिलक और ‘हरिहर’ की गर्जना के बीच, फिल्म की मंशा को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता.
यह फिल्म हमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी कहती है, जिनका वर्तमान राजस्थान और दिल्ली पर 12वीं सदी में राज था. गोरी को कई बार हराने के बाद आखिर में जिन्हें गोरी ने पराजित किया और अपना बंदी बना लिया.
पृथ्वीराज, संयोगिता के लिए जिनके प्रेम के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाता था, को कई दफा फिल्मों और टेलीविजन पर दिखाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के पोस्टर बॉय अक्षय कुमार अभिनीत हालिया फिल्म में जिस भव्यता के साथ उन्हें दिखाया गया था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था.
यहां कुछ बातें और हैं, जो पहेली बनकर सामने आती हैं- उन्हें आखिरी हिंदू सम्राट क्यों कहा गया है?
निश्चित तौर अगली कुछ शताब्दियों में कई और राजा हुए, जिन्हें हिंदुत्व ब्रिगेड धर्म के रक्षक के तौर पर पेश करता है (हालांकि यह भी काफी विवादित है). बाजीराव, तान्हाजी (दोनों 18 वीं सदी के) पर फिल्म बन चुकी है. और हमें आत्मबलिदान देने वाली पद्मावती (14वीं सदी) के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने खुद को दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में सौंपने की जगह जौहर करना चुना, जिनकी कहानी अतिनाटकीयता से भरपूर पद्मावत में सुनाई गई है.
इन सभी फिल्मों ने मुसलमानों को खल-कामी नायकों के तौर पर दिखाया और हिंदुओं का गौरवगान किया गया है, भले ही ऐसा करने के लिए उन्हें सती का महिमामंडन ही क्यों न करना पड़ा हो. इसके साथ ही हमारे जीवनकाल के दो हिंदू सम्राट- बाल ठाकरे और नरेंद्र मोदी पर भी फिल्में बन चुकी हैं.
बहरहाल, इशारों में बात कहने की परिपाटी को छोड़कर यह फिल्म जिस तरह बिना घुमाए-फिराए सीधे अपनी बात कहती है, वह हिंदी सिनेमा के हिसाब से एक मील का पत्थर है. और जहां एक तरफ यह भविष्य में और भी निर्लज्ज विज्ञापनों के लिए रास्ता तैयार करती है, वहीं दूसरी तरफ यह हिंदी सिनेमा और (भारतीय समझदारी) के लिए अतीत तक जाने वाले रास्ते को मजबूती से बंद कर देती है, जो पहले ही कपोल-कल्पना की मानिंद लगता है.
क्या वास्तव में ऐसा भी कोई समय था, जब भारत धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता था और भारत सरकार इसे प्रोत्साहित किया करती थी?
हिंदी फिल्मों में इन मूल्यों की झलक मिलती थी और हिंदू-मुस्लिम सौहार्द इनका एक नियमित विषय था. मुस्लिम चरित्र सामान्य तौर पर या तो एक रहमदिल चाचा या वफादार दोस्त या एक हसीन महिला का हुआ करता था. लेकिन यह कभी भी विलेन और उससे भी ज्यादा कभी गद्दार का नहीं हुआ करता था.
यह भी उतनी ही वास्तविकता से परे दृष्टि थी, लेकिन फिर भी यह किसी का नुकसान करने वाली नहीं थी और उन मूल्यों को दिखाती थी, जो हमारे अस्तिव में बसे हुए थे- या कम से कम हमें ऐसा नजर आता था.
डेढ़ दशकों के अंतराल की दो फिल्में हमें यह बताती है कि भारत कैसा था और लोकप्रिय संस्कृति में इसका प्रदर्शन कैसे होता था.
पहली फिल्म है धर्मपुत्र (1961), जिसका निर्देशन युवा यश चोपड़ा ने किया था, जिनके बेटे की कंपनी यशराज फिल्म्स ने अब सम्राट पृथ्वीराज का निर्माण किया है.
चोपड़ा ने महज दो साल पहले धूल का फूल फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपने करिअर का आगाज किया था, जिसका गाना तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, हर जुबां पर छा गया था.

धर्मपुत्र में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का एक कट्टरपंथी हिंदू के तौर पर बड़ा होता है, जो मुस्लिमों के खून का प्यासा है. लेकिन उसे बाद में यह जानकार धक्का लगता है कि वह खुद एक मुस्लिम की औलाद हो सकता है. हिंदी व्यावसायिक फिल्मों के लिए यह एक असामान्य विषय है, लेकिन यह अपने समय की राष्ट्रीय चेतना के पूरी तरह मेल खाती थी.
1977 में मसाला फिल्मों के बादशाह मनमोहन देसाई ने अमर अकबर एंथनी का निर्देशन किया. यह देसाई की दूसरी फिल्मों की तरह ही एक कमाई करने के लिए बनाई गई एक साधारण फिल्म थी, जिसमें उनके घिसे-पिटे फॉर्मूले की भरमार थी- बचपन में बिछड़े हुए भाई, असंभव से संयोग, दैवीय विधान और लोकप्रिय गाने.
अपने समय के एक नहीं बल्कि कई शीर्ष सितारों की मौजूदगी ने इस फिल्म में सोने पर सुहागा का काम किया. इस फिल्म का क्रेडिट एक तीनों जवान हो चुके भाइयों के सीक्वेंस के ऊपर चलता है, जिसमें वे एक कार के नीचे आ गई एक दृष्टिहीन महिला को खून दे रहे हैं और- एक और असंभव संयोग यह है कि- वह महिला और कोई नहीं, उन तीनों की मां है.
फिल्म के टाइटल कार्ड इनमें से हर एक पर आता है, जो अलग-अलग धर्मों को मानते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि फिल्म हमें याद दिलाती है, वे आपस में भाई हैं. फिल्म देखने वाले हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे बगैर नहीं रहता.
देसाई कोई कला फिल्मकार नहीं थे, लेकिन यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अपनी फिल्म के सेकुलर संदेश के जरिये वे, समीक्षकों को पसंद आने वाली किसी कला फिल्म निर्माता की किसी गंभीर फिल्म की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए.

अमर अकबर एंथनी अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली फिल्म नहीं थी, न ही देसाई की इसमें कोई दिलचस्पी रही होगी. वे शबाना आजमी से अक्सर अपने अभिनय में अतिनाटकीयता लाने के लिए कहा करते थे. उनका तर्क था कि उनकी फिल्में सत्यजीत रे की फिल्म नहीं है. लेकिन यह भारतीय दर्शकों के लिए एकदम उपयुक्त थी और आज भी लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं.
क्या इन दोनों में से कोई भी फिल्म आज बनाई जा सकती है और क्या हिंदुत्व के तथाकथित पहरेदार इन्हें बनाए जाने की इजाजत देते?
इस बात की गुंजाइश काफी कम है- अनियंत्रित हिंदुत्ववादी उन्मादियों को इनमें काफी कुछ आपत्तिजनक लगता. पहली फिल्म धर्मपुत्र, सिर्फ हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथ को ही कुपित नहीं करती, बल्कि किसी भी फिल्मकार में किसी ऐसी फिल्म में हाथ लगाने का साहस नहीं होता, जिसके कारण उसका भगवा गिरोहों के क्रोध का शिकार होना तय था.
एक उग्र मुस्लिम विरोधी दक्षिणपंथी को दिखाना, जो बाद में मुस्लिम निकलता है, हदों को पार करने वाला और भड़काऊ करार दिया जाता. बल्कि सच्चाई यह है कि इस मुख्य किरदार को एक हीरो के तौर, एक धर्म के रास्ते पर चलने वाले योद्धा के तौर पर दिखाया जाता, जो सही काम कर रहा है.
जहां तक दूसरी फिल्म का सवाल है कि तो इसके लिए भी मनाही होती. हिंदू-मुस्लिम-ईसाई के बीच भाईचारा? आज के भारत के लिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक विचार है.
और कुछ नहीं तो फिल्मों को सेंसर करने वाली उग्र भीड़ फिल्मकार को सभी को अंत में हिंदू धर्म में धर्मांतरित होते हुए दिखाने के लिए बाध्य कर देती, जबकि मनमोहन देसाई ने चतुराई से इस सवाल को अनुत्तरित छोड़ दिया. फिल्म में हिंदू हीरो एक देशभक्त होता, मुस्लिम करीब-करीब एक आतंकवादी, ईसाई लोगों का धर्मांतरण कराने वाला. अन्यथा धर्मरक्षकों की भीड़ इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देती.
कौन-सा गैरतमंद निर्देशक इन परिस्थितियों में फिल्म बनाना चाहेगा?
कोई चाहे तो यह तर्क दे सकता है कि सम्राट पृथ्वीराज एक छोटे से वक्फे के मूल्यों को दिखाती है, लेकिन क्या ये वास्तव में राष्ट्रीय मूल्य हैं या सिर्फ सत्ता और सरकारी तंत्र समर्थित हिंसक और शोर मचाने वाली भीड़ के मूल्य हैं, जिनका मकसद उनके हिंदुत्व को न मानने वाले लोगों पर अपनी इच्छा थोपना है.
भारतीयों की एक बड़ी संख्या धर्मपरायण हिंदू होने के बावजूद उनके हिंदुत्व में आस्था नहीं रखती. ये लोग भिन्न मत रखने वालों की लिंचिंग नहीं करते, न ही दूसरों को ऊंची आवाज में बोलकर चुप कराते हैं.
तो, हो सकता है कि सम्राट पृथ्वीराज के निर्माता और इसमें पैसा लगाने वालों झटका लगे. हो सकता है कि वे समझें कि वे सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादियों के भरोसे एक बहुत बड़े बजट की फिल्म से मुनाफा नहीं कमा सकते. उनमें से भी हर कोई थियेटर के बाहर कतार लगाकर खड़ा नहीं होनेवाला है.
अगर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े उम्मीद के अनुसार नहीं आए, तो सिनेमा का हिंदू ज्वार शांत हो जाएगा, जैसा कि हिंदी सिनेमा के कई अन्य मनपसंद विषयों के साथ हो चुका है.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)