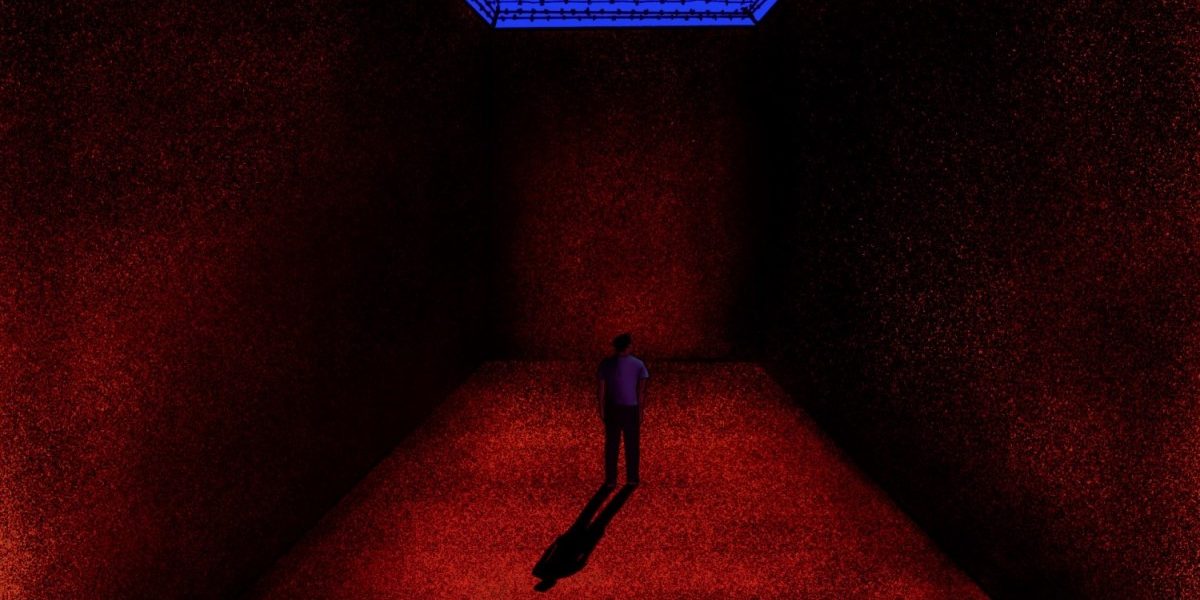गले से रुद्राक्ष की लंबी माला
लटक रही थी
जोगिया कलरवाले
कुर्ते पर …
दाहिने कान से
लाल फूल अटका पड़ा था,
चमक रहा था भाल पर
चंदन का पीला तिलक …
वो अपना रिक्शा
मेरे निकट ले आया
‘नमस्ते बाबाजी!’
संजीदगी में बोला—
‘किधर को ले चलूं बाबाजी?’
मैं उसको गौर से देखने लगा
वो अच्छा-भला युवक था,
गंदमी सूरत का दुबला-पतला!
बड़ी-बड़ी आंखें, सुरमई …
चौड़ी पेशानी पर
चमक रहा था चंदन का टीका
लुंगी पीली थी
पैर ख़ाली थे …
‘चलो बाबाजी
किधर ले चलूं?
छीपी तालाब?
बेगम पुल?’
कि इतने में
एक और युवक
इन कानों में
फुसफुसा के कह गया —
‘ख़बरदार, यह मुसलमान है …
इसके रिक्शे पर
कभी न बैठना आप!’
मगर अपना साथी
अ.अ. बोला —
‘हम इसी का रिक्शा लेते हैं.’
हमने उससे कहा—
‘हॉस्टल ले चलो,
हां, हां, मेरठ कॉलेज हॉस्टल.’
हमें हॉस्टल के गेट पर
पहुंचाकर
निहायत नरम आवाज़ में
वो कहने लगा —
‘बाबाजी, अब हम चुटैया भी रखेंगे
आठ-दस रोज़ की
भुखमरी के बाद
हमारे अंदर
य’अक्किल फूटी है!
बाबाजी,
रुदराछ के मनके
अच्छी मजूरी दिला रहे हैं
बाबाजी, अब हम
चुटला भी रखेंगे माथे पे
अब हम चंदन का टीका भी
रोज़ लगाते रहेंगे …
बाबाजी, अब हम
अपना नाम भी तो
‘परेम परकास’ बतलाते हैं …’
वो अपना रिक्शा लेकर
वापस जा रहा था …
उसने हमारी बातें सुन ली थीं
जभी तो
अपना ‘वक्तव्य’
सूत्र-रूप में
हमारे सामने रख गया था
अपना रिक्शा लेकर
प्रेमप्रकाश जा रहा था
और हम दोनों
मिनटों में उसे जाते हुए
देखते रहे …
… …
यों तो वो
कल्लू था …
कल्लू रिक्शावाला
यानी कलीमुद्दीन …
मगर अब वो
‘परेम परकास’
कहलाना पसंद करेगा …
कलीमुद्दीन तो
भूख की भट्ठी में
ख़ाक हो गया था
‘जियो बेटा प्रेम प्रकाश!
हां, हां,चोटी ज़रूर रख लो
और हां, पूरनमासी के दिन
‘गढ़ की गंगा में डूब लगा आना!
हां, हां, तेरा यही लिबास
तेरे को रोज़ी रोटी देगा!
सच बेटा प्रेम प्रकाश
तूने मेरा दिल जीत लिया!
लेकिन तू अब इतना
ज़रूर करना
मुझे उस नाले के क़रीब
ले चलना कभी
उस नाले के क़रीब
जहां कल्लू का कुनबा रहता है!
मैं उसकी बूढ़ी नानी के पास
बीमार अब्बा जान के पास
बैठकर चाय पी आऊंगा कभी!
कल्लू के नन्हे-मुन्ने
मेरी दाढ़ी के बाल
सहलाएंगे …और …’
‘और?’
और तेरा सिर! …’
मेरे अंदर से
एक ग़ुस्सैल आवाज़ आई …
‘बुड्ढे, अपना इलाज करवा!
तेरी खोपड़ी के अंदर
गू भर गई है!
खूसट कहीं का!
कल्लू तेरा नाना लगता है न?
ख़बरदार साले
तुझे किसने कहा था
मेरठ आने के लिए? …
लगता है
वो ग़ुस्सैल आवाज़
आगे भी कभी-कभी
सुनाई देती रहेगी …
नागार्जुन की इस कविता का शीर्षक है ‘तेरी खोपड़ी के अंदर’. कविता क्या है, एक फटकार है या नागार्जुन के हृदय में निकली चीत्कार! या भारत को एक भयानक चेतावनी या उसके लिए भविष्यवाणी. स्वतंत्रता के बाद विकसित हुए भारतीय जीवन पर एक फटकार.
कविता में एक व्यर्थ की भावुकता हो सकती थी जिसे नागार्जुन के कुशल कवि ने जैसे बिल्कुल पोंछ दिया है. उपहास का स्वर है लेकिन उसका पात्र है कल्लू उर्फ़ प्रेम प्रकाश से सहानुभूति दिखलाने वाला बाबा.
कविता यह नहीं बतलाती कि आख़िर कल्लू यानी कलीमुद्दीन ने क्यों प्रेम प्रकाश बनने का फ़ैसला किया होगा? आठ-दस रोज़ की भुखमरी उसे क्यों झेलनी पड़ी होगी? और भुखमरी से निकलने का यही तरीक़ा क्यों उसने चुना होगा? कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश में ख़ुद को बदल लेने का? क्यों चुटिया और टीका और रुद्राक्ष के मनके उसे अच्छी मजूरी दिला रहे हैं?
कविता यह कारण नहीं बतलाती है क्योंकि वह मानती है कि भारतीय पाठकों की सांस्कृतिक या सामाजिक या राजनीतिक या जनतांत्रिक स्मृति मेरठ का एक अर्थ जानती है. जैसे जबलपुर, भिवंडी का, जमशेदपुर का, भागलपुर का, नेल्ली का, हाशिमपुरा का, अहमदाबाद का, मुज़फ़्फ़रनगर का. ये सारे नाम सिर्फ़ शहरों के नाम नहीं, मील के पत्थर हैं भारतीय जनतंत्र के पथ के.
भारतीय जनतंत्र मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा के सहारे या उसके बावजूद इस रास्ते पर आगे बढ़ता गया है. ये सारे शहर उस हिंसा के प्रतीक हैं. यह हिंसा इन शहरों को बनाती, बदलती है. इन शहरों की बनावट, बसाहट को, उसमें रह रहे लोगों के बीच के रिश्तों को वह हिंसा बदलती है.
कविता सिर्फ़ कल्लू का जो कि अब प्रेम प्रकाश है, ‘वक्तव्य’ सुनाती है. वह तो बतिया रहा है अपनी सवारियों से, लेकिन जो वह बोल रहा है उसे कविता उसका ‘वक्तव्य’ कहती है. वक्तव्य जो कि औपचारिकता का आभास देता है. जैसा वक्तव्य सरकार देती है या राजनेता या अफ़सर देते हैं. यह हिंसा के शिकार एक मुसलमान का वक्तव्य है. यह वक्तव्य है या टिप्पणी है उस भारत पर जहां भूख से बचने का यही रास्ता बच गया है कल्लू या कलीमुद्दीन के पास?
यह कविता मुझे बार-बार याद आती रही है. चंडीगढ़ के मेरे मित्र ने अपनी एक टैक्सी यात्रा के बारे में जब बतलाया, यह कविता याद आई. टैक्सी ड्राइवर ने अपना नाम सोनू बतलाया था. सफ़र के अंत में किराया लेने के लिए उसने अपना फ़ोन नंबर दिया. मित्र ने जब उस नंबर पर भुगतान कर दिया तो उसकी रसीद मिली. फ़िरोज़ को उनका दिया पैसा मिल गया था. मेरे मित्र ने फ़ोन की स्क्रीन देखी और खामोशी से टैक्सी से उतर गए. उन्होंने नागार्जुन की यह कविता नहीं पढ़ी थी.
रिक्शे पर ख़रामा-ख़रामा चलते हुए हमारे कवि ने परेम परकास से उसके रहने की जगह, उसके घर-ख़ानदान का हाल चाल ले लिया था. हमारे मित्र को मालूम था कि इसके बारे में उनकी कोई भी जिज्ञासा सोनू उर्फ़ फ़िरोज़ को उनके इरादे के बारे में आशंकित कर सकती है.
यह कविता याद आई जब इंदौर में हिंदुओं की गली में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को बुरी तरह पीटा गया. यह इल्ज़ाम लगाकर कि वह नाम बदलकर हिंदू औरतों को धोखे से चूड़ी बेच रहा था. तस्लीम को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसकी जमानत की अर्ज़ी ज़िला अदालत ने ख़ारिज कर दी. कोई 4 महीने बाद उसे उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल पाई.
तस्लीम के वकील ने ज़मानत देने की अदालत की इस मेहरबानी के लिए उसका और भारतीय जनतंत्र के संविधान का शुक्रिया अदा करते हुए वक्तव्य दिया: ‘उच्च न्यायालय के जमानत के आदेश ने साबित कर दिया है कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है. यह संविधान की जीत है.’
कविता फिर याद आई जब पढ़ा कि कर्नाटक के धारवाड़ में नुग्गीकेरी मंदिर के सामने तरबूज़ा बेचते हुए नबीसाब किल्लेदार का ठेला गुंडों ने उलट दिया. फिर याद आई जब जबलपुर में अमित शुक्ला ने जोमाटो के डिलीवरीमैन का नाम फ़ैयाज़ मालूम होने पर अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया. फ़ैयाज़ का वक्तव्य था,’हां, तकलीफ़ तो हुई. अब क्या बोलेंगे सर, …गरीब लोग हैं …सहना पड़ेगा.’
और तब भी, कविता को याद किया जब पढ़ा कि लोग आधार कार्ड देखकर मुसलमान सब्जीवालों को अपने मोहल्ले या कॉलोनी में घुसने से मना कर रहे हैं.
तब भी यह कविता याद आई जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का वक्तव्य पढ़ा कि गुवाहाटी में मियां मुसलमानों को सब्जी और मसाला नहीं बेचने दिया जाएगा.
अनुज लुगुन ने सम्मिलित नागरिकता की मांग की है, सम्मिलित नागरिकता जो श्रमशील नागरिकता भी है. अगर रोज़ी में, श्रम में शिरकत नहीं है तो नागरिकता में भी शिरकत कैसे होगी?
हर हिंसा के बाद शहर, क़स्बे बंटते हैं. 40 साल पहले कलीमुद्दीन ने आख़िरकार प्रेम प्रकाश का भेस लिया जिससे वह जी सके:
यों तो वो
कल्लू था …
कल्लू रिक्शावाला
यानी कलीमुद्दीन …
मगर अब वो
‘परेम परकास’
कहलाना पसंद करेगा …
कलीमुद्दीन तो
भूख की भट्ठी में
ख़ाक हो गया था
नागार्जुन कल्लू को उसकी इस हिकमत के लिए जो शाबाशी देते हैं, वह वास्तव में अपने मुल्क को लानत है.
कवि यह जानने के बाद कल्लू के कुनबे में जाना चाहता है, वहां चाय पीना चाहता है. धारवाड़ में फल बेचने वाले किल्लेदार को वहां की साहित्य सभा के उद्घाटन का न्योता दिया गया. जबलपुर में जोमेटो ने अमित शुक्ला को जवाब दिया कि फ़ैयाज़ की जगह वह किसी हिंदू को उनके पास खाना लेकर नहीं भेजेगा. वे नागरिकता की फाड़ दी गई चादर की सिलाई कर रहे हैं.
जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंदर से ग़ुस्सैल आवाज़ आती है –
‘अपना इलाज करवा!
तेरी खोपड़ी के अंदर
गू भर गई है!
खूसट कहीं का!
कल्लू तेरा नाना लगता है न?’
नागार्जुन की कविता ख़त्म इस आशंका पर होती है,
लगता है
वो ग़ुस्सैल आवाज़
आगे भी कभी-कभी
सुनाई देती रहेगी …
इस ग़ुस्सैल आवाज़ का जवाब कैसे दिया जाएगा, इसी से हिंदुस्तान के जनतंत्र के सफ़र का वर्तमान और भविष्य तय होगा.
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)
(इस श्रृंखला के सभी लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)