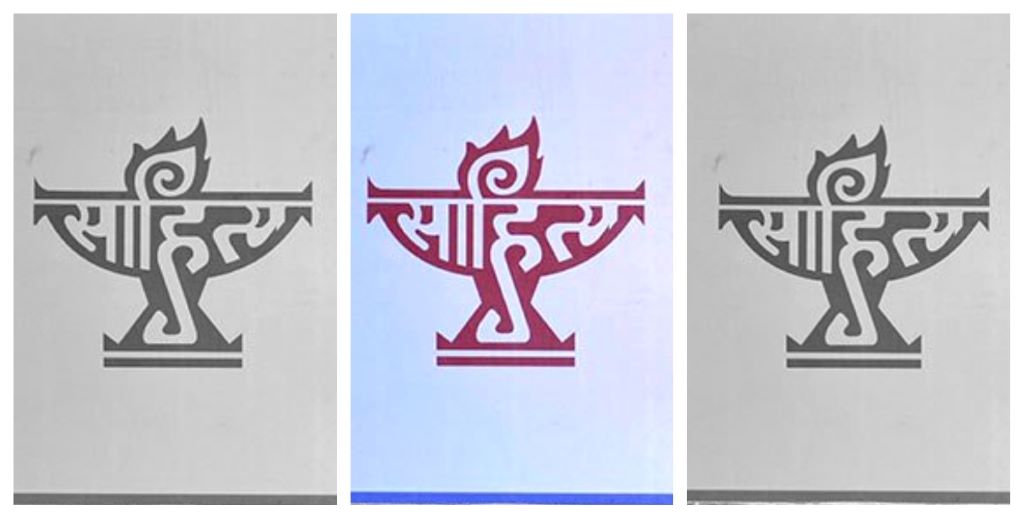जब तब के प्रधानमंत्री साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष थे तो अकादेमी द्वारा नियुक्त जूरी ने महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी में अपने पुरस्कार के लिए चुना, उनकी पुस्तक ‘मध्य एशिया का इतिहास’ के लिए. चूंकि उस समय कम्युनिस्टों की धर-पकड़ हो रही थी जो ‘अधूरी आज़ादी’ कह रहे थे तो अकादेमी ने यह पुरस्कार इस आधार पर रोक लिया था कि राहुल जी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और उन्हें यह दिया जाए या नहीं तय करने के लिए मामला अकादेमी के अध्यक्ष को भेजा.
नेहरू जी ने वैचारिक मतभेद को खारिज़ करते हुए यह निर्णय लिया कि जूरी की सिफ़ारिश को मानते हुए पुरस्कार दिया जाए और राहुल जी को पुरस्कार मिला. उससे पहले नेहरू जी यह स्पष्ट कह चुके थे कि प्रधानमंत्री नेहरू साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष नेहरू के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
एक और वाकया 90 के दशक का है. अकादेमी का पुरस्कार, कांग्रेस सरकार के रहते, एक वर्ष किसी पंजाबी लेखक की किसी पुस्तक को दिया गया था जिसमें इंदिरा गांधी की सख़्त निंदा की गई थी. मामला संसद में उठा और उस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री अर्जुन सिंह ने वह वक्तव्य दिया था कि यद्यपि सरकार उस चुनाव से अपने को अलग करती है, यह अकादेमी का निर्णय है, जो एक स्वायत्त संस्थान है और सरकार उसकी गतिविधियों और निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती.
इधर जो हुआ है कि इस वर्ष के अकादेमी पुरस्कार एक प्रेस वार्ता में घोषित किए जाने के पहले संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर रोक लिए गए कि मंत्रालय से उनका अनुमोदन होना है. हवाला दिया गया है कि पिछली जुलाई में सभी अकादेमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कोई क़रारनामा (मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) हुआ था जिसके अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी पुरस्कार योजनाओं का पुनर्गठन करना है. जब तक यह नहीं हो जाता और उसे मंत्रालय अनुमोदित नहीं कर देता तब तक अगर कोई पुरस्कार दिए जाएंगे तो वे मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ही.
सो अब अकादेमी और साहित्य जगत् को इस अनुमोदन का इंतज़ार करना होगा. यह अकादेमियों की स्वायत्तता को सीधे अवमूल्यित करना है और सीधे-सीधे अकादेमी के लेखक-सदस्यों, जूरी के लेखक-सदस्यों और पुरस्कार के लिए अनुशंसित लेखकों सभी का एक साथ अपमान है.
मुझे अकादेमी पुरस्कार 1994 में मिला था जूरी में नरेश मेहता और श्रीलाल शुक्ल थे. मैंने 2015 में कुछ अन्य भारतीय लेखकों के साथ देश में बढ़ती असहिष्णुता और अकादेमी द्वारा अपने ही पुरस्कृत लेखकों की हत्या पर शोकसभा तक न करने के विरोध में यह पुरस्कार लौटा दिया था.
उससे पहले मैं दो बार अकादेमी के हिंदी पुरस्कार का निर्णय लेने वाली जूरी का सदस्य था. दोनों बार निर्णय बहुमत से लिया गया, सर्वसम्मति से नहीं.
मेरे साथ एक बार राजेन्द्र यादव और विश्वनाथ तिवारी और दूसरी बार केदारनाथ सिंह और लीलाधर जगूड़ी थे: पहली बार राजेन्द्र यादव निर्णय से असहमत थे, दूसरी बार मैं. पुरस्कार कुंवर नारायण और राजेश जोशी को मिले. जूरी की सिफ़ारिश बंधनकारी मानने की प्रथा थी और कार्यकारिणी ने शायद ही कभी उसमें कोई फेरबदल किया हो.
संस्कृति मंत्रालय में, उसके समूचे इतिहास में बहुत कम लेखक या साहित्यविद् अधिकारी रहे हैं. उसकी साहित्य संबंधी विशेषज्ञता उसके अंतर्गत दो संस्थानों साहित्य अकादेमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में है. अब यह स्पष्ट नहीं है कि संस्कृति मंत्रालय किस विशेषज्ञता का सहारा लेकर अपनी ही असल विशेषज्ञ अकादेमी के निर्णय का अनुमोदन करेगा या उसे रोक लेगा. मामला प्रशासनिक नहीं, साहित्यिक है.
अनुमोदन से याद आया कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उस समय हर वर्ष ‘भारत भारती पुरस्कार’ के अलावा सत्तर से अधिक वार्षिक पुरस्कार देता था. मुख्यमंत्री उसकी पदेन अध्यक्ष थीं. इन पुरस्कारों के लिए बाक़ायदा जूरी नियुक्त हुईं और उन्होंने लेखक और पुस्तकें चुनीं. अनुमोदन के लिए फाइल लगभग एक वर्ष मुख्यमंत्री की मेज़ पर लंबित रही. मुख्यमंत्री ने कुल शायद पांच पुरस्कार अनुमोदित किए और बाक़ी सत्तर से अधिक खारिज़ कर दिए और आदेश दिए कि पुरस्कारों की संख्या कम की जाए.
मुझे जब भारत भारती पुरस्कार दिए जाने की ख़बर फ़ोन पर किसी अधिकारी ने दी मैंने स्वीकृति दे दी. बाद में पता चला कि इन 70 से अधिक पुरस्कारों को ख़ारिज किए जाने का, तो मैंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया. 2004 में जब मध्य प्रदेश सरकार का कबीर सम्मान मुझे दिया गया था तो जूरी की सिफ़ारिश ‘अनुमोदन’ के लिए छह महीनों तक मंत्री के पास लंबित रही थी.
तो साहित्य अकादेमी के पास अनुमोदन कब आएगा या आएगा भी कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता. यह नोट करने की बात है कि इस घटना को लेकर व्यापक लेखक समाज में और मीडिया में कोई ख़ास खलबली नहीं है.
एक प्रश्नावली
जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो प्रश्न मैंने उठाए उनकी एक सूची पेश है.
लोकतांत्रिक संकुचन, ज्ञान की अवज्ञा, झूठ के निज़ाम और हिंसा-घृणा-हत्या-अन्याय की दैनिकता के समय में क्या साहित्य सच बोलने की चेष्टा कर रहा है?
क्या अंतःकरणहीन होते जा रहे समाज में साहित्य सजग अंतःकरण बना-बचा हुआ है?
राजनीति के, राज्य के हर क्षेत्र में घुसपैठिया होने के भयाक्रान्त माहौल में क्या साहित्य जीवन को उसकी अदम्य बहुलता, अपार विविधता में, निर्भय होकर, दर्ज़ कर पा रहा है?
क्या साहित्य आज ‘आत्मा का गुप्तचर’ है? क्या सुनियोजित विस्मृति के अभियान के बरक़्स साहित्य याद कर रहा है, याद दिला रहा है, याद को बचा रहा है?
क्या हर कहीं सफलता की अंधी दौड़ के परिवेश में साहित्य में सार्थकता और विफलता की जगह अब भी बची हुई है?
क्या साहित्य अपने नाम के अनुरूप आज हमारा सहचर है और अपने स्वभाव के अनुरूप आज ‘सत्याग्रह’ कर रहा है, ‘सविनय अवज्ञा’ के शिल्प में है और ‘असहयोग’ कर रहा है?
क्या आज सच्चे, ईमानदार और साहसी साहित्य की नियति अपने समय और समाज के विरोध में होना है?
आज साहित्य की चुप्पियां क्या हैं?
क्या साहित्य की संरचनाएं जैसे संस्थाएं, अकादेमियां, हिंदी विभाग, हिंदी अध्यापक, लेखक संघ आदि साहित्य के सत्याग्रह में शामिल हैं, प्रश्नवाचकता और प्रतिरोध में साथ हैं या अप्रसांगिक हो गए हैं?
क्या सार्वजनिक वित्तीय समर्थन के संकीर्ण-संकुचित होते जाने से रंगमंच को अपनी निर्भीक प्रश्नवाचकता से विरत होना पड़ रहा है?
क्या रंगकर्म में लगे अनेक छोटे समूहों ने, अक्सर छोटे शहरों-कस्बों में, अभाव की रणनीति बनाकर साहस, प्रश्नांकन, नवाचार, कल्पना आदि को सजीव रखा है?
परंपरा की अधम दुर्व्याख्या के दौर में क्या रंगमंच परंपरा के जीवंत तत्वों, अंतर्विरोधों और विडंबनाओं, उदात्तता और अतिचारों, संभावनाओं का अन्वेषण कर पा रहा है?
क्या आज रंगमंच सहमति, बहुलता, प्रश्नांकन और नैतिक निर्भयता का मंच है?
शास्त्रीय कलाओं में क्या यह मीडियोक्रिटी, मूर्धन्यों की अनुपस्थिति का पठार समय है? क्या निरंतर संकीर्ण और सांप्रदायिक होता जा रहा सार्वजनिक समर्थन शास्त्रीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है?
क्या नवाचार, परंपरा का पुनराविष्कार, सूक्ष्मता, जटिलता की साधना और अभिव्यक्ति शिथिल पड़ रही है?
क्या शास्त्रीयता को निरी शोभा में घटाकर उसके मर्म और धर्म को क्षत-विक्षत किया जा रहा है?
क्या शास्त्रीयता की सदियों के आरपार विकसित ‘एकलता’ ‘सामूहिकता’ में बलात बदली जा रही है?
क्या शास्त्रीयता भूलती जा रही है कि वह सदियों से संस्कृति की बहुलता की वाहक और औपनिवेशिकता का प्रतिरोध रही है?
क्या लोकप्रियता का दबाव सार्थकता को हाशिये पर ढकेल रहा है?
क्या बिना आलोचना और बढ़ती विचारहीनता शास्त्रीयता को खोखला कर रही है?
क्या शास्त्रीयता राजनीतिक विद्रूप-घृणा-हिंसा-अत्याचार को देखते हुए बंदनयन भक्ति में क़ैद है?
ललित कलाएं सार्वजनिक कला-संस्थानों, जैसे केंद्रीय और राज्य अकादेमियों के अप्रासंगिक हो जाने के कारण, क्या पूरी तरह से बाज़ार पर निर्भर हो गई हैं? क्या बहुत सारी कला आजकल निरी डिज़ाइन में बदल रही है और उसे अर्थ की हानि की परवाह नहीं है? कला की ज़्यादातर आलोचना अंग्रेज़ी में लिखी जाती है और बहुत कम भारतीय भाषाओं में? ऐसा क्यों? क्या अंग्रेजी आलोचना में भारतीय कला चिंतन और अवधारणाओं का आधुनिक पुनराविष्कार की अनुपस्थिति स्वयं कला में उत्तराधिकार की बढ़ती विस्मृति का ही संस्करण है?
ज़्यादातर आलोचना अमूर्तन के बजाय आख्यानमूलक कला पर क्यों एकाग्र रहती है?
दिल्ली से लेकर अनेक राजधानियों, बड़े शहरों में सड़कों के दोनों ओर चाहरदीवारियों, मेट्रो के खंभों आदि पर बेहद भौंडी, कुरुचिपूर्ण सार्वजनिक कला चित्रित की जा रही है- जो न लोक है, न आधुनिक. सामान्य नागरिकों के कला-बोध को वह विक्षत-दूषित कर रही है. भोथरा और सतही बना रही है. इसका कलाकार, उनके समूह और संस्थाएं विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं?
यों तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, साधन-संपन्न और प्रभावशाली, सत्ताभक्ति में, झूठ-नफ़रत-हिंसा-झूठ ख़बरें फैलाने में बहुत सक्रिय है और उसे अक्सर संस्कृति के लिए समय और जगह निकाल पाना मुश्किल होता है. जैसे राजनीति संस्कृति की उपेक्षा करती है वैसे ही मीडिया भी.
कई दशकों तक रंगमंच-ललित कलाओं-संगीत-नृत्य आदि की आधुनिक आलोचना ज़्यादातर अख़बारों में ही शुरू और सक्रिय रही है. अनेक आलोचक वहीं से उभरे. पर अब जैसे राजनीति के लिए संस्कृति मात्र शोभा रह गई है वैसे ही मीडिया के लिए भी. सब कुछ दृश्य भर है इस तर्क से तस्वीर छपती है. आलोचना या समीक्षा नहीं.
क्या मीडिया की कोई सांस्कृतिक भूमिका और ज़िम्मेदारी भी होती है? क्या वह भी उसे अनुष्ठानों में घटाकर अपना संस्कार या संस्कारहीनता व्यक्त करने लगा है?
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)