पिछले लगभग एक दशक से व्यवस्था और समाज के कमोबेश हर स्तर पर मुस्लिमों को अलग-थलग करने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है. उनके ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में आम मुसलमान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ख़ुद को कहां पाता है?

मोदी सरकार के आने के बाद से भारत में मुस्लिमों के साथ अकस्मात तौर पर लेकिन लगातार हो रही संगठित हिंसा इस हद तक पहुंच चुकी है, जहां देश का आम मुस्लिम अपनी ज़िंदगी और आजीविका बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान को लेकर लगातार डर के साये में जी रहा है.
गूगल सर्च में ‘इंडियन मुस्लिम इन फियर’ (डर के साये में भारतीय मुसलमान) लिखकर सर्च कीजिए, तो साल 2015 में यूपी के दादरी में मोहम्मद अख़लाक़ की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद से हर साल लिखे गए इस तरह के दर्जनों लेख और रिपोर्ट्स दर्ज हैं- कहीं पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान है, तो कहीं कोई अभिनेता देश के हालात पर चिंता जता रहा है. कहीं उत्तर प्रदेश में हेट क्राइम (नफरत के चलते किए गए अपराध) में मारे गए पीड़ितों के परिवार की इंसाफ की लड़ाई है, कहीं सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर छोड़ रहे मुस्लिमों का दर्द. जो सिलसिला एक मुस्लिम घर के फ्रिज में रखे मीट पर उठे संदेह से शुरू हुआ था, वो अब किसी ‘वजह’ का मोहताज नहीं रहा है. किसी दिन कोई सिरफिरा बंदूक उठाकर आपको बस आपके होने की वजह से गोली मार देगा और आप बयानों और घटना के वीडियो का फैक्ट-चेक करके बताते रह जाएंगे कि उसकी हरकत सालों से पल रही नफ़रत का नतीजा थी, किसी क्षणिक आवेश का नहीं.
बीते कई सालों से दर्ज हो रहा ये ख़ौफ़ अब आम मुसलमानों के ज़ेहन में गहरे से बस चुका है और वे अपनी जान बचाने के लिए अपने तौर-तरीके, रहन-सहन में बदलाव करने को मजबूर हैं. भय का हाल ये है कि इस रिपोर्ट के लिए बात करने वाले लगभग हर व्यक्ति ने उनका नाम और पहचान न ज़ाहिर करने की शर्त रखी है.
मूल रूप से पटना की रहने वाली सारा* कहती हैं, ‘ट्रेन की घटनाओं (पहले लिंचिंग और हालिया गोलीबारी) ने हमें अंदर तक झकझोर दिया है. सबसे पहले तो हमने ट्रेन में खाना ले जाने से बचना शुरू कर दिया था और अगर खाया भी तो हम इस बात को लेकर सतर्क रहते हैं कि किसी को यह मीट न लगे. कई बार तो ऐसा भी होता है कि खाने की बजाय हल्का-फुल्का खा के ही सफर ख़त्म कर लिया.’
‘जयपुर एक्सप्रेस की घटना के बाद मेरे परिचित एक बुजुर्ग जोड़े ने ट्रेन के बजाय फ्लाइट से टिकट बुक करवाया. वे उम्रदराज़ हैं और इस तरह के सफर का तजुर्बा न होने के कारण इसे लेकर सहज नहीं हैं, और फिर इसमें खर्चा भी ज्यादा है. लेकिन सच यही है कि लोग ट्रेन में सफर करने से बच रहे हैं.’
ट्रेन में सफर को लेकर डर और खानपान पिछले कई सालों में बढ़ा है. यूपी की रहने ज़ेबा* पहले दिल्ली में पढ़ती थीं और अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, ‘मैं हॉस्टल में रहती थी तो घर से आते वक्त थोड़ा ज़्यादा खाना लाया करती थी. मुझे कबाब परांठा पसंद था लेकिन फिर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया कि टिफिन में ये नहीं ले जाना है. ये बदलाव आज से चार-पांच साल पहले ही हो गया था. अब तो लोगों का रवैया दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है.’
लोगों के रवैये को लेकर ज़ेबा ने एक क़िस्सा बताया, ‘ये अभी कुछ साल पहले की ही बात है, मैं ट्रेन से दिल्ली आ रही थी. मैं बुर्का, नक़ाब या हिजाब नहीं पहनती हूं यानी देखकर कोई मेरे धर्म के बारे में नहीं जान सकता. पर नाम का आप कुछ नहीं कर सकते. तो उस दिन पास में एक कपल बैठे थे और उनकी एक छह-सात साल की बच्ची थी जो मेरे साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी. उसी दौरान उसने मेरा नाम पूछा और मैंने बिना कुछ सोचे बता दिया. उसने फ़ौरन कहा- आप मुसलमान हैं, मैंने कहा- हां, जिस पर वो उसी रौ में बोली- आप यहां क्यों रहती हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं जातीं. मैं अवाक् रह गई, मुझे समझ ही नहीं आया इस बात का क्या जवाब दूं. उसके बाद रास्ते भर न उसके माता-पिता न उसने मुझसे बात की.’
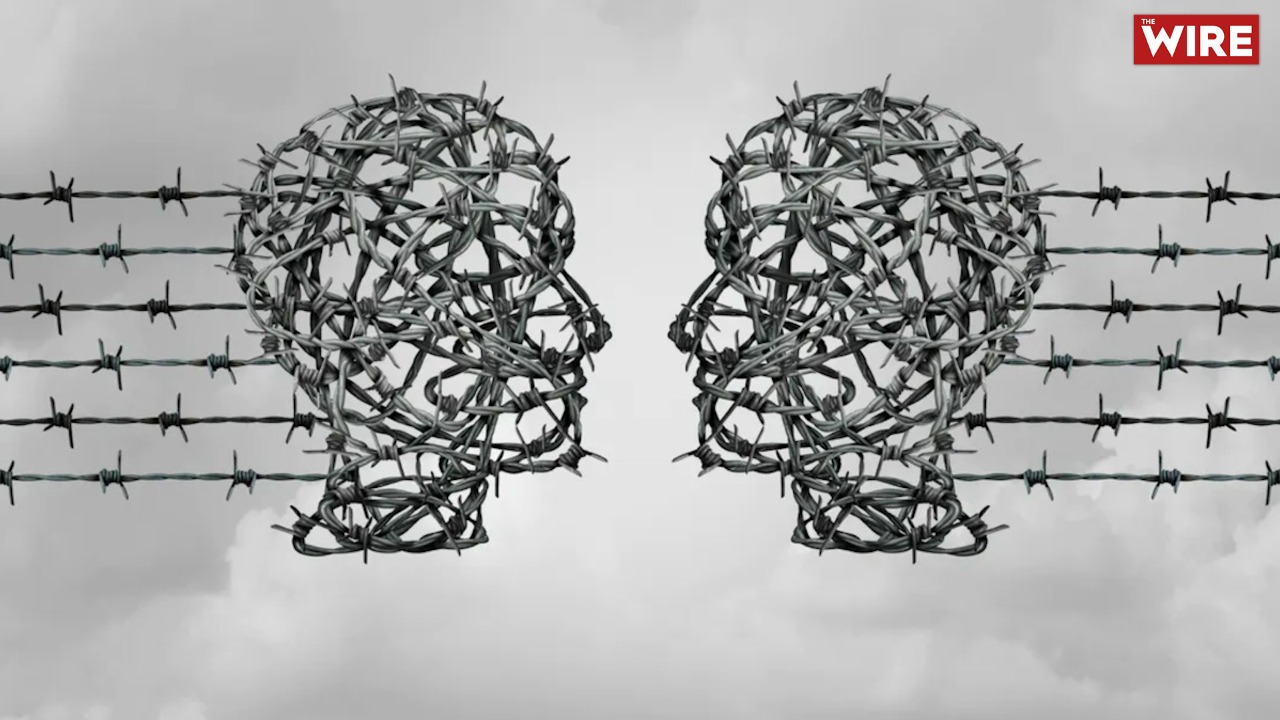
डर किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं
पत्रकार राना अयूब संभ्रांत तबके से आती हैं लेकिन बीते दिनों उन्होंने परिजनों की धार्मिक पहचान को लेकर चिंता को सोशल मीडिया पर साझा किया. जयपुर एक्सप्रेस हत्याओं के बाद चार अगस्त को इंस्टाग्राम पर राना ने अपने पिता के बारे में लिखा था कि वे किस तरह जुमे को पास की मस्जिद में सफ़ेद कुरता-पजामा और टोपी लगाकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वे उनके सुरक्षित होने के बारे में डरती हैं.
उनकी इस पोस्ट पर साढ़े सात सौ के क़रीब कमेंट्स हैं, जिनमें अधिकतर में इसी तरह के डर और किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनाए गए तरीके लिखे हैं. एक यूज़र ने लिखा है कि जब उनका कोई परिजन या रिश्तेदार बस या ट्रेन में होता है, तब वे फोन पर उनसे सलाम या ख़ुदा हाफ़िज़ कहने से बचती हैं. पश्चिम बंगाल के एक छात्र ने बताया है कि उनकी क्लास में अधिकांश हिंदू हैं और कभी कभी वे ‘जय श्री राम’ जैसे नारे लगाते हैं, जिसके चलते उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है.
राना की ही तरह लेखक रख़्शंदा जलील भी उच्च वर्ग से हैं और अपने प्रिविलेज (विशेषाधिकारों) से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं. द वायर पर प्रकाशित एक लेख में उन्होंने बताया है कि आम मुस्लिमों में फैले डर और मानसिक अवसाद ने किसी भी वर्ग को भी नहीं बख़्शा है. लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे दक्षिणी दिल्ली के एक पॉश इलाके में वे एक बिल्डिंग में घर देख रही थीं, जिसके पास एक पुरानी मस्जिद थी और उस इमारत के हर फ्लोर पर केवल मुस्लिम परिवार रहते थे. लेकिन कई बार वहां जाने के बाद भी वे उस घर को खरीदने के लिए अपना मन नहीं बना सकीं.
वे लिखती हैं, ‘वहां उस बिल्डिंग पर एक अदृश्य ‘X’ था. मस्जिद से नजदीकी, पूरी तरह से गैर-मुस्लिम इलाके में हर मंजिल पर रहते मुस्लिम परिवार ने मुझे अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी और वहां हुई हत्याओं की याद दिला दी. मेरे दोस्तों ने मज़ाक भी उड़ाया कि मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूं, वो गुजरात की बात है ये दिल्ली है वगैरह-वगैरह…
… लेकिन मैं मुझे मिले हर प्रिविलेज- शिक्षा, वर्ग, ‘बड़े पदों पर बैठे दोस्तों के- के बावजूद ये स्वीकार करती हूं कि मुझे डर लगता है, इतना जो पूरी ज़िंदगी में नहीं लगा. मैं 60 साल की हूं और इस भयानक डर को स्वीकार करती हूं, जो मेरे सीने पर किसी असहनीय बोझ की तरह है और कभी-कभी मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर देता है.’
जिन सारा का ज़िक्र ऊपर किया गया है, वे उच्च आयवर्ग के परिवार से आती हैं. उनका डर भी राना अयूब के डर की ही तरह है. वे कहती हैं, ‘पहले शुक्रवार का इंतज़ार रहता था, अब शुक्रवार आते ही चिंता घेरने लगती है कि कहीं किसी मस्जिद में कोई घटना न हो जाए. एक दिन पापा और भाई को जुमे की नमाज़ से लौटने में थोड़ी देरी हुई तो मैं सचमुच घबरा गई. पापा मस्जिद में जुमे की नमाज़ के लिए जाते वक़्त कभी भी अपना मोबाइल नहीं ले जाते थे. अब हम उनसे कहते हैं कि फोन लेकर जाएं. थोड़ी-सी देर हुई नहीं और हम कॉल करना शुरू कर देते हैं.’
‘मुझसे पहले मेरा धर्म पहुंच जाता है’
शौक़त* भारतीय रेलवे में काम करते हैं और इससे ज्यादा पहचान नहीं बताना चाहते. वे आमतौर वही कपड़े पहनते हैं, जिन्हें मुस्लिमों की वेशभूषा का ‘स्टीरियोटाइप’ बताया जाता है- कुरता-पजामा और दाढ़ी. वे कहते हैं, ‘देखिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सियासी माहौल है, लेकिन हम जैसे लोग जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उन्हें मज़ाक़ के लहजे में भी ये सुनने को मिल जाता है कि मियां जी रेलवे में कैसे? वो कई बार हमारे होने के बहाने हमारी सलाहियत पर भी सवाल उठाते हैं. असल में रोज़मर्रा में शामिल बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जहां लोगों के व्यवहार से लग जाता है कि इनके सामने मुझसे पहले मेरा धर्म पहुंचा दिया गया है.’
उन्होंने आगे बताया, ‘ऐसे ही अगर संयोग से किसी सेक्शन में दो-चार भी मुसलमान कर्मी हों तो बातें होने लगती है कि ये सेक्शन तो पूरा पाकिस्तान बना हुआ है. और कई बार सामने से कह दिया जाता है कि तुम्हीं लोगों का राज है. एक दो बार ये बातें इस तरह से भी सामने आई हैं कि हमारे घर की महिलाएं जब विभाग के किसी कार्यक्रम में शामिल होती हैं तो उनके लिबास या स्कार्फ़ आदि के बारे में दूसरी महिलाएं कह देती हैं कि अब इस ज़माने में इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है. मतलब हमारे लिए कोई न कोई बात उनके ज़ेहन में चल रही होती है.’
मुस्लिम पहचान को लेकर पूर्वाग्रहों और डर की जड़ें साल दर साल गहरी ही हो रही हैं. एक एनजीओ में काम करने वाले ओसामा बताते हैं, ‘मैं हुलिए से मुसलमान मालूम देता हूं. तो जब कई बार सफ़र करता हूं तो शायद इसी वजह से ही लोग ऐसे वीडियो तेज़ आवाज़ में चलाने लगते हैं जिसमें भड़काऊ भाषण जैसा कुछ होता है. कई बार ये भी महसूस किया है कि ट्रेन में मुस्लिम परिवार की मौजूदगी से दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा असहज हो जाते हैं और डरे हुए भी लगते हैं. एक बार सफर में था कि घर से भाई का फ़ोन आया, तो मैंने आदत के मुताबिक़ सलाम किया तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ऐसे मत करो. मैं राजस्थान जा रहा था जहां उस समय हिंदू-मुस्लिम तनाव जैसा माहौल था तो भाई ने इसे लेकर भी कहा कि स्टेशन पर उतरकर किसी को अपना नाम नहीं बताना है, ज़रूरी हो तो कोई दूसरा नाम बताना.’
अरीब* कॉरपोरेट जॉब करते हैं और कोलकाता में रहते हैं. आसपास के लोगों के मुस्लिमों को लेकर पूर्वाग्रहों के बारे में वो बताते हैं, ‘हमारे जानने वालों में दूसरे समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन अब उनकी बातचीत में मुसलमानों के लिए एक अलग तरह की राय को महसूस होती है, जैसे एक दोस्त ने किसी बातचीत के दौरान एक ख़ास तरह के पेशेवर काम के बारे में कहा कि क्या बताएं अब इस काम में इतना मुसलमान सब आ गया है कि और वो किसी भी रेट पर जैसे-तैसे काम कर ले रहा है, मार्केट ही खत्म कर दिया है! मैं बाद में सोचता रहा कि क्या इस बातचीत में ‘मुसलमान’ कहने की ज़रूरत थी.’
‘लेकिन हाल ये है कि मुसलमान अपने ख़िलाफ़ नफ़रत की इसी मानसिकता के साथ रहने को अभिशप्त हैं, मुसलमानों के लिए अपने आप अघोषित नियम बन गए हैं- कि कहीं भी हों, सफ़र भी कर रहें हो तो अपने आप में सिमटकर रहने में ही कुछ भलाई है. पता नहीं सामने वाला कब आपको टारगेट कर ले.’
गैर-मुस्लिम लोगों के रवैये में आए बदलावों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शारिब* ने भी महसूस किया है. उन्होंने बताया, ‘मैं अक्सर लगातार सफ़र में रहता हूं, पढ़ाई के दौरान भी ऐसा ही था. तब स्लीपर क्लास में चलता था और कभी महसूस नहीं किया कि मैं मुसलमान हूं और मुझे किसी और नज़र से देखा जा रहा है, जैसे सब सफ़र करते थे वैसे ही मैं भी करता था. देखता था कि लोग वहां नमाज़ भी पढ़ लेते थे. मुझे निजी तौर पर उस समय ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लोग इसका बुरा नहीं मानते थे बल्कि जगह दे देते थे कि आप पढ़ लीजिए. उनकी नमाज़ होने तक लोग आदर भाव से आपस में बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज अगर अपनी बर्थ पर भी कोई नमाज़ पढ़ता है तो लोग बुरा मान जाते हैं, मोबाइल निकलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं.’
उन्होंने आगे कहा, ‘पहले हम लोग ट्रेन में सबसे बातें करते थे और यही इसका लुत्फ़ था लेकिन अब मुझे डर लगता है. अब जब तक सामने वाला कोई बात नहीं करता हम उसे टोकने से भी डरने लगे हैं, ये दूरी क्यों पैदा हो रही है, ज़ाहिर है कि हमारे बारे में बड़े पैमाने पर एक राय बनाई गई है. और तो और मैं अपने मुस्लिम दोस्तों, जानने वालों से सख्ती से कहता हूं कि ट्रेन में खाना लेकर जाओ ही मत, किसी बहस में हिस्सा मत लो, लिबास के मामलों में मैं अपनी बहनों के साथ सख्ती करने लगा हूं कि हिजाब मत पहनो और वैसे ही दिखो जैसे नॉन-मुस्लिम दिखते हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम डरे हुए हैं ये बस इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए. हम कुछ और नहीं कर सकते तो किसी हद तक अपनी पहचान के साथ ही समझौता कर ले रहे हैं.’
औरतों के लिए बढ़ी चुनौतियां
भारतीय परिवारों में महिला के अधिकारों, उनकी आज़ादी की बात उतनी ही होती है जितनी सहूलियत से ‘अफोर्ड’ की जा सके. आमतौर पर महिलाएं या लड़कियां जिन परेशानियों का सामना एक महिला होने के चलते करती हैं, अब मुस्लिम महिलाओं के लिए उसमें उनकी पहचान भी शामिल हो गई है. उनके आने-जाने, पढ़ने-लिखने, नौकरी करने जैसे फैसले पहले ही मुश्किल थे, अब उनमें मज़हबी पहलू और जुड़ गया है. पीयूसीएल की एक रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बीच हज़ार लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी. ख़बर यह भी आई है कि जयपुर एक्सप्रेस में गोलीबारी करने वाले चेतन सिंह चौधरी ने एक बुर्का पहनी महिला से बंदूक की नोंक पर ‘जय माता दी’ बोलने को कहा था.
लेकिन क्या मसला सिर्फ धार्मिक पहचान या हिजाब का है? जवाब नोमान* देते हैं. दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े नोमान फ़िलहाल बिहार की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वे बताते हैं, ‘हाल की घटनाओं के बाद से महिलाओं को लेकर रवैये में फर्क तो आया है, पहले हम सिर्फ उनके औरत होने के लिहाज़ से उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करते थे, अब इसमें ‘मुस्लिम’ होना और जुड़ गया है. मेरे घर की एक बच्ची का कॉलेज में एडमिशन होना था, तो ऐसा कॉलेज चुना गया जो घर से पास हो. इसी तरह एक रिश्तेदार के यहां हुआ. उनकी बेटी का नाम एक नामी कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आ गया था, लेकिन वो कॉलेज घर से सात-आठ किलोमीटर दूर था. उनके घर के बड़े इसके लिए तैयार नहीं हुए और पास के ही एक कॉलेज में नाम लिखवा दिया गया.’

नक़ाब, बुर्क़े या हिजाब पहनने वाली महिलाएं भी ऐसे ही डर से दो-चार हैं. दरभंगा की इमराना ख़ातून गृहणी हैं, और बताती हैं, ‘अब बुर्क़ा पहनकर घर से बाहर निकलने में डर-सा लगता है, ख़ुदा-न-ख़्वास्ता मौजूदा माहौल में अगर किसी तरह का तनाव हो जाए तो हमें आसानी से पहचाना जा सकता है. ऐसे ही ट्रेन में साथ वाले लोग कैसे हैं इसको लेकर चिंता रहती है, और अब ज़्यादा होने लगी है कि अपनी पहचान को कैसे और कितना छुपाएं. हमारे मज़हब में जो चीज (पर्दा) महिला सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी आज हमारे लिए असुरक्षा का कारण बनता जा रहा है.’
रेहाना* दिल्ली में रहती हैं और फ्रीलांस तौर पर मीडिया से जुड़ी हुई हैं. वो कहती हैं, ‘मैं हिजाब पहनती हूं लेकिन मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अधिकांश समय घर से काम करती हूं. मेरे पास ये विकल्प है लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी नौकरियों में हैं जहां रोज़ बाहर जाना होता है और आज के माहौल में मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बड़ी चुनौती है.’
रेहाना सही हैं, नौकरी पर जाने या घर से काम करने का चुनाव हर किसी को नसीब नहीं है. मधुबनी की नबीला* प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं. उनका कहना है, ‘हमें आज तक सामने से किसी ने खुले तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसी व्यवहार और बातचीत में कभी कोई बात खटक जाती है और हम ख़ुद ही अपने ऊपर एक दवाब महसूस करने लगे हैं. अभी पिछले दिनों विभागीय प्रशिक्षण के लिए गई थी, आदत के अनुसार बुर्क़ा पहन रखा था, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र में जाने से पहले मैंने इस बात का ख़याल रखा कि इसे उतार दूं और ये सब करते हुए मुझे लग रहा था कि कोई देख रहा है, इसलिए जल्दी-जल्दी इसे उतारकर अंदर चली जाऊं.’
वे आगे कहती हैं, ‘शायद ये मेरा अपना वहम हो या आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन जाने-अनजाने घर से निकलते हुए अपनी पहचान को छिपाने की एक कोशिश करने लगी हूं, रही बात डर की तो ये सब मेरे लिए किसी अदृश्य दुनिया को अनुभव करने जैसा है. मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो किसी तरह की धार्मिक पहचान को न अपनाए, जो करना है उसे अपने घर के अंदर तक सीमित रखा जाए.’
महिलाओं के हिजाब उनकी नौकरी के लिए घातक भी साबित हुए हैं. नई दिल्ली की शायला इरफ़ान शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाया करती थीं, लेकिन अचानक उन्हें एक रोज़ कहा गया कि उनके विद्यार्थियों और अभिभावक उनके हिजाब को लेकर सहज नहीं हैं, इसलिए वे इसे न पहनें. शायला ने नौकरी छोड़ दी. उनका कहना था कि अगली नौकरी के इंटरव्यू में भी उन्हें कहा गया कि वो हिजाब हटाएंगी तो नौकरी मिलेगी.
पुणे की डेंटिस्ट लुबना आमिर की भी समान कहानी है. पढ़ाई में अव्वल रहने के बावजूद मुस्लिम पहचान उनके नौकरी मिलने के रास्ते में आई. एक बड़े डेंटल क्लीनिक उन्हें नौकरी देने के लिए हिजाब हटाने को कहा. लुबना ने इनकार कर दिया और अपने क्लीनिकल काम के सपने को छोड़कर एक बायोइन्फरमेटिक्स कंपनी में नौकरी करने लगीं. उन्होंने अल-जज़ीरा से बातचीत में कहा, ‘उन्हें हमारे मुस्लिम होने से परेशानी है, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी हमारे मुस्लिम दिखने से है.
घरों की चौखट पर अनजाने डर का साया
रख्शंदा के लेख में वो एक जगह कहती हैं कि इस तरह के डर को महसूस करने वाली वो अकेली नहीं हैं और उन्हें शहरी भारतीयों की ख़ामोशी में इस डर की परछाई देखी है. वो कहती हैं, ‘…मैं उनकी चुप्पी में इसे सुन सकती हूं, उनके किसी राजनीतिक बहस में पड़ने से फ़ौरन इनकार में ये डर दिखता है, किसी सांप्रदायिक मसले पर की गई सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की जल्दी में यह डर नज़र आता है, स्कूल, कॉलेज आदि के वॉट्सऐप ग्रुपों में फैलती नफ़रत के प्रति उदासीन होने में दिखता है…’
डिजिटल इंडिया का एक कड़वा सच यह भी है कि वॉट्सऐप ग्रुप सांप्रदायिक ज़हर के घर-घर पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. किसी भी अपार्टमेंट या सोसाइटी का वॉट्सऐप ग्रुप सुबह से ही ऐसे धार्मिक संदेशों की आड़ में सप्लाई हो रही नफ़रत का बड़ा केंद्र हैं.
दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले परिचित के सोसाइटी के ग्रुप में लगातार मुस्लिमों के ख़िलाफ़, फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेजेज़ आते हैं, इस ग्रुप में यहां रहने वाले दो-एक मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं. शुरुआत में कुछ लोगों और उन मुस्लिम सदस्यों ने फ़र्ज़ी ख़बरों के फैक्ट-चेक साझा किए, वेरीफाई की हुई सामग्री दिखाई, लेकिन सांप्रदायिक संदेशों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई. हारकर अब वे कुछ नहीं कहते.
मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का आलम यह है कि इस साल रमज़ान के दौरान नोएडा की बड़ी सोसाइटी में प्रबंधन की इजाज़त के साथ एक जगह पर नमाज़ पढ़ने का विरोध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया था. इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक व्यक्ति की निजी संपत्ति में तरावीह पढ़े जाने को लेकर बजरंग दल के लोगों ने हंगामा खड़ा किया था. मामला पुलिस तक पहुंचा था और पुलिस ने संपत्ति मालिक को ही सामूहिक प्रार्थना आयोजित करने से मना कर दिया था.
ऐसे द्वेषपूर्ण माहौल में रह रहे मुस्लिम परिवार अपने पड़ोसी या आसपास के लोगों पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं हैं.

मुस्लिमों के लिए डरना फ़िज़ूल नहीं है
पिछले कई सालों में मुस्लिमों के इस डर, हर पल बढ़ते संशय को ख़ारिज करने की कोशिश की गई है, हिंदुत्वपंथी नेता उन्हें ‘न डरने’ की नसीहतें देते नज़र आते हैं. हालांकि मुसलमान इससे कतई इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता.
शौकत कहते हैं, ‘आज ब्रेनवाश किया जा चुका है, मीडिया हर वक़्त ज़हर उगल रहा है, तो ऐसे माहौल में अंदर से बहुत अच्छा तो महसूस नहीं होता. अब आप इसे डर कह लीजिए या कुछ और एक चिंता जाने-अनजाने लगी रहती है. न्यू इंडिया में ये ज़्यादा खुले अंदाज़ में मुसलमानों के साथ हो रहा है और उनके व्यक्तित्व में इस मनोवृत्ति को शामिल कर दिया गया है. हम ये नहीं कह सकते कि ये डर और चिंता काल्पनिक है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है.’
सारा ने इस माहौल की उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की बात कही. वे बताती हैं, ‘मुझे किसी सांप्रदायिक दंगे में फंसे होने और बिल्कुल बेबस होने के सपने आने लगे हैं. मैंने ये बात मम्मी और कुछ दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि उनके साथ भी यही हो रहा है.’
रेहाना मुस्लिमों के साथ हुई हिंसा के बाद हुए असर के कुछ सामाजिक पहलू भी गिनाती हैं. वे कहती हैं, ‘जहां तक मैंने देखा-समझा है अब जो मुस्लिम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अपनी गाड़ी या हवाई जहाज़ से चलने को प्राथमिकता दे रहे हैं. लोग हिंदू बहुल इलाकों निवेश नहीं करना चाहते, हमले के डर से हिंदू बाज़ारों में खरीदारी से बच रहे है. दुकानदार उर्दू में बोर्ड या मुस्लिम नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. घरों या सोसाइटी में छोटे-मोटे काम करने वाले मुस्लिम लोगों ने हिंदू इलाके या सोसाइटी में जाना कम कर दिया है.’
शारिब जोड़ते हैं, ‘हमारी ज़ेहनी हालत ऐसी बना दी गई है कि हम चार लोग इकठ्ठे होकर चाय पीते हुए और कुछ बात ही नहीं करते, बस इसी तरह की ख़बरों की चर्चा करने लग जाते हैं, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करने लगे हैं. बस ये समझिए कि हम अपने वजूद में उलझा दिए गए हैं.’
रख़्शंदा ने इस डर को इस तरह बयां किया है, ‘मैं मुस्लिम नहीं दिखती, तो एक हद तक शायद मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरे नाम का क्या? रेलवे के बुकिंग चार्ट में इसे कैसे छिपा सकती हूं? या किसी ने पहचान पूछी तो? … अगर मुस्लिम खून की प्यासी भीड़ मुझे घेर ही लेती है तो क्या अंग्रेज़ी बोलकर बच पाऊंगी, मेरे तथाकथित प्रिविलेज धरे के धरे रह जाएंगे और मैं ये सोचकर ही कांप जाती हूं.’
अरीब के लिए ये सारे बदलाव केवल आज या कल की बात नहीं हैं. उनका कहना है, ‘ये सब मंसूबाबंद सियासत के तहत हो रहा हैं. एक बात ये भी है कि भारतीय समाज तेज़ी से ऐसा होता चला जा रहा है कि अगर किसी को उसके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है या जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई आपके बचाव में नहीं आएगा. सियासत इसी मानसिकता से खेल रही है. अगर कल को केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं भी रहती है तो इस नफ़रत और मानसिकता से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है.’
क्या मेरा पहचान लिया जाना ख़तरनाक है?
फ़ैयाज़ अहमद वजीह द वायर उर्दू के असिस्टेंट एडिटर हैं. इस बारे में पूछने पर कहते हैं, ‘मैं अपने आसपास की सहमी हुई ख़ामोशी को इन दिनों ज़्यादा महसूस करने लगा हूं, इस ख़ामोशी में शोर बहुत है, लेकिन लोग ऐसा दिखलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक है. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने हुलिए और दूर से पहचान ली जाने वाली वेशभूषा को लेकर चिंतित हैं, जयपुर एक्सप्रेस हत्या मामले के बाद ये चिंता और बढ़ी है. ऐसे में मुझे ये बात परेशान करती है कि शायद कुछ लोग अपनी दाढ़ी हटा लें, नक़ाब न ओढ़ें, लेकिन वो लोग क्या करेंगें जो मदरसों में पढ़ते हैं, मौलाना हैं या इमाम हैं? क्या वो इस तरह के किसी डर को अपने अंदर महसूस करके ऐसा कोई क़दम उठा सकते हैं? ’
‘मैं इन बातों को मुस्लिम समुदाय का डर न भी कहूं तो आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या एक मुसलमान के तौर पर मुझे भी किसी दिन पहचाना जा सकता है, और मेरा पहचान लिया जाना ख़तरनाक है. इस डर के बारे में कम लोग बात करना चाहते हैं, एक तरह की ख़ामोशी ओढ़कर बहुत सारे मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को पीछे रखने लगे हैं.’
‘मुसलमानों को लगता है कि जब भी उन्हें मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जाता है या जाएगा तो दूसरे समुदाय के लोग यहां तक कि पुलिस भी उनके बचाव में नहीं आएगी. इसके बावजूद मैं यहां उम्मीद की बातें भी कर सकता हूं, लेकिन स्टेट ने जिस तरह से नफ़रत की सरपरस्ती की है, धर्म संसद में जिस तरह से नरसंहार की बातें की गई हैं, इन सबको देखते हुए उम्मीद की किरण बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती. मुसलमानों को सत्ता के लिए नफ़रत की भेंट चढ़ाया जा चुका है.’
(* परिवर्तित नाम)
(फ़ैयाज़ अहमद वजीह के सहयोग के साथ)




